स्वतंत्रता दिवस पर विशेष
संसद की सर्वोच्च्ता का सच
संसद की सर्वोच्च्ता का सच
गोविन्द श्रीवास्तव/अनंत जौहरी
हम संसद को सर्वोच्च् मानकर लगातार उसे और शक्तिशाली बनाने की कामना करते हैं । लेकिन वास्तविकता एक दूसरी ही सच्चई की ओर इशारा कर रही है । संसद को विदेशी मामलों, विदेशी व्यापार, विदेशों में से होने वाली संधियों आदि के संबंध में बहुत ही सीमित अधिकार हैं । इतना ही नहीं हमारे देश के विकास को दिशा देने वाली पंचवर्षीय योजनाआें को भी संसद से स्वीकृत करवाना अनिवार्य नहीं है । यानि हम एक प्रशासनिक सत्ता तंत्र में रह रहे हैं।
आजकल यह चर्चा आम है कि सांसद, संसद और सरकार में स्वतंत्र और सर्वशक्ति सम्पन्न कौन है ? लोकपाल मसौदा समिति के प्रस्ताव पर आने वाली प्रतिक्रिया ने इस मूल प्रश्न को व्यापक रूप से उठा दिया है ।
अलग-अलग देखे तो लगता है कि इनमें से प्रत्येक स्वतंत्र भी है और सर्वशक्तिमान भी । सांसदों का दो तिहाई बहुमत कानून बनाता है । संसद वह सर्वोच्च् संस्था है जिसके कानूनी निर्णय को सर्वोच्च् न्यायालय भी नहीं बदल सकता । जबकि संंसद संविधान में संशोधन कर सकती है । जब संविधन की शक्तियों के परिप्रेक्ष्य में देखे तो लगता है कि संविधन का उल्लघंन तो हो ही नहीं सकता और सभी निर्णय संविधान की धाराआें के अनुसार ही होते हैं । लेकिन व्यवहार में देखे तो कोई भी सरकार अध्यादेशों के जरिये रातो-रात सर्वोच्च् न्यायालय के हाथ बांध देती है ।
सरकार किसी भी पार्टी की हो, संविधान ने उसे इतने व्यापक अधिकार दे रखे हैं कि वह विदेशों से ऐसी भी संधि कर सकती है कि उसे मालूम भी हो कि किस कंपनी या व्यक्ति का कितना काला धन विदेशों में जमा है पर वह उस संधि के हवाले से कह देगी कि हम जानते है पर बताएंगे नहीं । संविधान प्रदत्त अधिकारों के आधार पर किसी भी सरकार को, विदेशी समझौते एवं संधि करने की व्यापक शक्ति प्राप्त् है । इसी आधार पर बहुचर्चित परमाणु समझौते के समय लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी को यह राज खोलना पड़ा था कि संसद में परमाणु समझौते पर बहस तो हो सकती है परन्तु मत विभाजन नहीं हो सकता । उसी समय भी विपक्ष के द्वारा यह मांग उठाई गई थी कि संविधान की इस धारा को बदला जाए ।
संसद के अधिकार को कार्यपालिका द्वारा सीमित करने के बार में लेखक व राजनीतिक कार्यकर्ता सुनील का कहना है भारतीय संविधान, विधायिका (संसद और विधान सभाआें) के अधिकार की सीमा तय कर देता है, जिसके चलते कार्यपालिका विधायिका से ज्यादा ताकतवर बन जाती है । यह चारित्रिक विशेषता भी भारतीय संविधान में १९३५ के ब्रिटिश भारत सरकार के कानून से विरासत में ली गयी है । संघीय सूची में विदेशों के साथ संधियां व समझौते, विदेशों के साथ व्यापार, विदेशी कर्ज आदि विषय आते है । इन विषयों पर संसद की राय नहीं ली जाती ।
विदेशी संबंधों, विदेश व्यापार, वाणिज्य, विदेशी कर्ज आदि पर कार्यपालिक का पूरा नियंत्रण रहता है । विश्व व्यापार संगठन के डंकल प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करते समय भी इस विषय पर बहस नहीं कराई गई थी कि भारत को इस पर ह्स्ताक्षर करने चाहिये या नहीं । संविधान संसद को व्यवहारत: आर्थिक नीतियों के संदर्भ में कोई अधिकार नहीं देता । देश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में नीतियां बनाने और लागू करने पर पूरा नियंत्रण कार्यपालिका का है ।
संसद बाह्य या आंतरिक कर्ज के संदर्भ मेंकुछ नहीं बोल सकती । अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय या बहुपक्षीय आर्थिक समझौतों या उसके साथ आर्थिक रिश्तों के बारे में हस्तक्षेप करने का संसद को कोई अधिकार नहीं ।
पंचवर्षीय योजना पर संसद का कोई नियंत्रण नहीं है । शुरूआती पंचवर्षीय योजनाआें में परम्परागत तौर पर योजना को मात्र सुझावों के लिए चर्चा के लिये नहीं संसद के सामने रख दिया जाता था । अब तो इस परम्परा को भी छोड़ दिया गया है ।
समय-समय पर घोषित की जाने वाली आर्थिक नीतियों जैसे आयात-निर्यात नीति, औघोगिक नीति आदि पर संसद कुछ नहींबोल सकती ।
महात्मा गांधी ने इसी संसदीय लोकतंत्र के बारे में१९०९ में हिन्द स्वराज्य में कहा था कि पार्लियामेन्ट की मां ब्रिटिश संसद का ढांचा ऐसा है कि वह कोई बड़ा जनहितैषी निर्णय नहीं ले सकती है । हमारे संविधान पर भी इसलिये ब्रिटिश संविधान की पूरी छाया है । दिखने में सरकार बहुत शक्तिशाली है परन्तु वास्तव में इसकी नकेल मुख्यतया सत्ता पक्ष के राजनैतिक दल के हाथ में होती है । लेकिन यह भी आभास ही है और यही दोषपूर्ण लोकतंत्र का परम सत्य है । सामान्यत: सभी राजनैतिक दलों के शीर्ष में निर्णायक शक्ति या तो एक छोटे से समूह के पास या उस पार्टी के एक व्यक्ति (सुप्रीमो) के पास होती है ।
लेकिन क्या कोई भी एक व्यक्ति या राजनैतिक दल के शीर्ष मेंबैठे निर्णायक कुछ व्यक्तियों का समूह इतना शक्तिशाली हो सकता है ? शायद आज की राज्यव्यवस्था में ऐसा संभव नहीं है । मूर्त रूप में सरकार या सुप्रीमो इतने शक्तिशाली दिखते हैं, लेकिन वास्तव में इनकी संचालक शक्ति तो वित्तीय पूंजी के वर्चस्व वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिये बड़े पैमाने पर अरबों खरबों का भ्रष्टाचार करती है और छोटे भ्रष्टाचारियों को अपने उत्पाद व सेवाएं बेचती हैं । इनके प्रभाव में राजनैतिक दल, सरकारें और सांसद आदि अक्सर जनविरोधी निर्णय लेते है ।
जन लोकपाल के आग्रही समूह ने इसे आजादी की दूसरी लड़ाई भी कहा है । यह एक मूल प्रश्न है कि क्या हमारी आजादी की लड़ाई अधूरी रह गई ? आजादी की लड़ाई इसलिये थी कि जनता को उसकी सार्वभौम सत्ता वापस मिले । वह अपनी अर्थव्यवस्था के लिये स्वयं निर्णय करते हुए अपने नियंत्रण का तंत्र, खड़ा कर सके । संसदीय लोकतंत्र की बुनियाद जनता का चुना, प्रतिनिधि लोकसभा का सासंद है । इस मौलिक इकाई की स्वतंत्रता दलबदल विधेयक ने छीन ली । क्योंकि इसके बाद वह जनता के प्रति उत्तरदायी, निर्देशित न होकर अपनी पार्टी द्वारा आदेशित हो गया । वह भय व लालच द्वारा संचालित किया जाता है । पिछले ४२ साल में आठ बार लोकपाल विधेयक पेश हुआ परन्तु पारित नहीं हो पाया क्योंकि सत्ता कभी भी अपने उपर नियंत्रण नहीं चाहती है । शासकीय लोकपाल विधेयक में इसीलिए सांसद को भ्रष्टाचार करने में सुरक्षा देने की कोशिश की गयी है ।
संसद को अगर गंगा जैसी पवित्र नदी कहा जाये तो सूरदास ने कहा है - एक नदिया एक नार कहावत मैलो जलहि भरयो । तीनों मिल जब एक संग भै, सुरसरि नाम परयो । नदी में नाला और मैला जल थोड़ा-थोड़ा मिलने पर भी उसे गंगा कहा गया, परन्तु आज पवित्र नदियों में इतना प्रदूषण हो गया है, इतना मैला जा रहा है कि नदियां पूर्णत: प्रदूषित हो चुकी हैं, यही हाल आज की संसद का हो रहा है । जो कतिपय, जनहितैषी, प्रबुद्ध एवं जुझारू सांसद हैं वे भी नक्कारखाने में तूती की आवाज की स्थिति में जा चुके है । वे भयभीत है उनके ऊपर चुप रहने का लेबल लगा हुआ है और वे जानते है कि अगर बहुत आदर्शवादी बनेंगे तो अगली बार टिकिट ही नहीं मिलेगा । अधिकांश संस्थाएं उद्देश्य के विपरीत कार्य कर रही है । इसके साथ हम देख रहे है कि संस्थाआें को निरन्तर कमजोर किया जा रहा है । जनपक्षधर, नौकरशाह प्रताड़ित किये जाते हैं, संस्थाआें में केन्द्रीकरण है और सर्वोच्च् पदाधिकारी को विवेकाधीन अधिकार प्राप्त् हो गए हैं ।
शासकीय प्रस्ताव में प्रधानमंत्री को लोकपाल के अंकुश से मुक्त रखना इसी केन्द्रीय शक्ति को तानाशाही की शक्ति देना है । दूसरी और जनता के अधिकार को यानि उसके प्रतिनिधि सांसद को संसद में चुप रहने के लिये बाध्य करना इस संसदीय लोकतंत्र के ढांचे का मूल षड़यंत्र है ।
स्वतंत्रता के पश्चात् के इन वर्षो में हम देखते है कि गणतंत्र में तंत्र ही मजबूत होता जा रहा है और गण निरन्तर कमजोर हो रहा है । किसी भी लोकतंत्र के स्थिति उत्तम नहीं कही जा सकती है । लोकतंत्र के लिए सामान्य जन एवं संसद दोनों को ही मजबूत करना होगा । अतएव ऐसे प्रयासों के लिए देहात से लेकर दिल्ली तक अभियान चलाना होगा ।




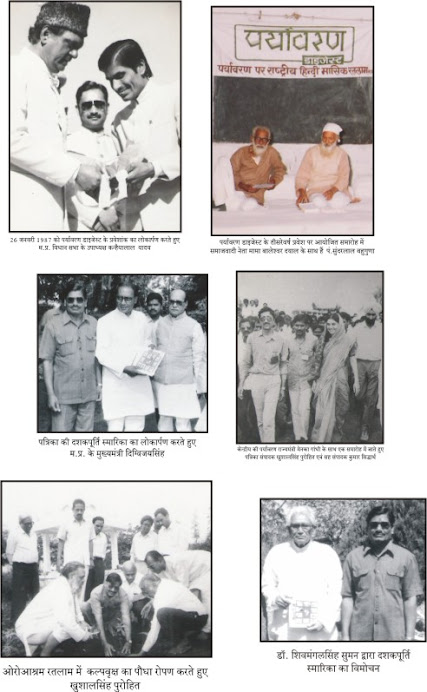



कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें