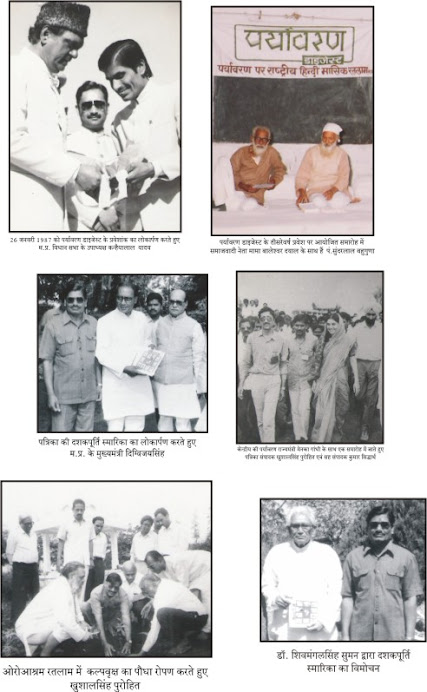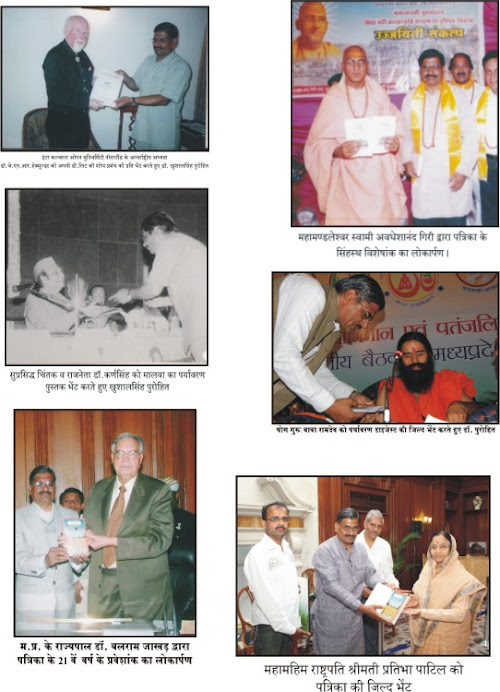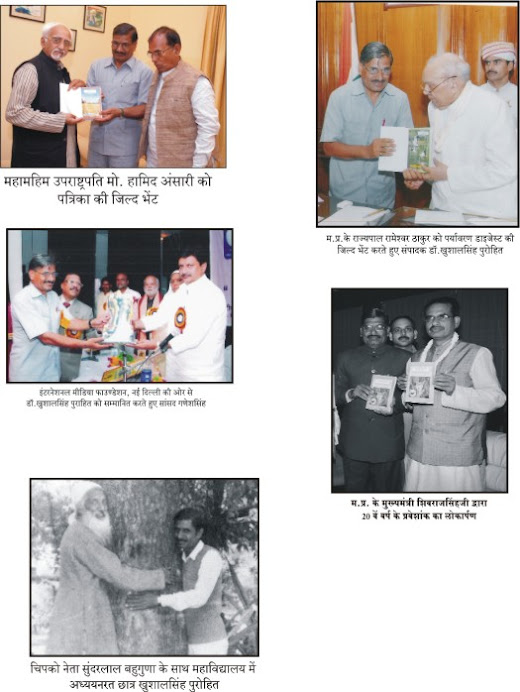मंगलवार, 15 अप्रैल 2008
सम्पादकीय
प्रसंगवश
१ सामयिक
२ विज्ञान जगत
३ विशेष लेख
४ जनजीवन
५ प्रदेश चर्चा
६ खास खबर
७ आवरण कथा
८ पर्यावरण परिक्रमा
पर्यावरण के लिये बदल रहे हैं अंग्रेज
जलवायु परिवर्तन के संभावित खतरोंको कम करने के प्रयासों में ब्रिटेन की सबसे बड़ी सफलता यह रही हैं कि आम लोगों ने इस चुनौती को स्वीकार किया है । लंदन में ९० फीसदी लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करने लगे है । पर्यावरण को लेकर लोग अपने व्यवहार में बदलाव ला रहे है । जबकि सरकार की तरफ से दो क्षेत्रों में बेहद अच्छा काम हुआ है, पहला कम ऊर्जा खपत वाली ग्रीन बिल्डिंगों का निर्माण और दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हाइब्रिड और स्वच्छ इंर्धन को बढ़वा देना । पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने भारी निवेश किया है । इन दोनों में सरकार को अगले कुछ साल में और अच्छे परिणामों की उम्मीद है । लेकिन अब सरकार के लिए असली चुनौती कोयला आधारित बिजलीघरों से होने वाले काबनडाई आक्साईड उत्सर्जन मेंे कमी लाने की है। ब्रिटिश सरकार के ताजा आंकड़ो के अनुसार अभी कार्बनडाई आक्साईड का सर्वाधिक ३५ फीसदी उत्सर्जन कोयला आधारित बिजलीघरोंसे होता है । जबकि वाहनों की हिस्सेदारी २२ फीसदी है । वायु एवं समुद्री परिवहन का उत्सर्जन करीब सात फीसदी है । इन क्षेत्रो में एक साथ कई प्रयास किए जा रहे हैं । वायु यातायात में कार्बन उत्सर्जन पर करों को दोगुना किया गया है । इसी प्रकार पेट्रोलियम पदार्थोंा की कीमतों में टैक्सों में बढ़ोतरी की गई जो ६४-६७ फीसदी तक पहुंच चुके है । डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट के लो कार्बन व्हीकल शोध विभाग के प्रमुख रोय कोलिन बताते है कि ब्रिटेन मेें २४ लाख कारें है जिनमें हाइब्रिड कारों की संख्या बढ़कर १७ हजार से भी ऊपर पहुंच चुकी है । हाईब्रिड कारों पर शोध जारी है । पहले चरण में इस पर २० मिलियन पौंड का बजट रखा गया था जिसे अब बढ़ाकर ५० मिलियन पौंड किया जा रहा है । इसी प्रकार यहां ग्रीन बिल्डिंगें तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं । ग्रीन भवनों और हाइब्रिड वाहनों के लिए सरकार की तरफ से करों आदि में छोटी-बड़ी रियासतें भी दी गई हैं । लेकिन कोयले से बिजली उत्पादन को हतोत्साहित करने के मुद्दे पर ब्रिटेन सरकार को अहम फैसला लेना है । तमाम विकसित देश इसके खिलाफ है लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस दिशा में अपना रूख स्पष्ट नहीं किया है । माना जा रहा है कि सरकार इस बारे में जल्द अपनी स्थिति साफ करेगी ।
नमूना तकनीक से बाघ संरक्षण को नई दिशा
सेंटर फार वाइल्ड लाइफ स्टडीज (बेंगलूर) के निदेशक और वन्य प्राणी विशेषज्ञ डा. उल्लास कारंथ का मानना है कि भारतीय वन्य प्राणी सस्थान (डब्ल्यू आई आई) ने पहली बार नमूना तकनीक से बाघों की सही आबादी का पता लगाया है । वन विभाग और पर्यावरणविद बरसों से बाघ के पंजो के निशानों (पगमार्क) से गणना किया करते थे, जिसमें अनेक गलतियों और फेरबदल की गुंजाईश रहती थी । कैमरा पद्धति के उपयोग और गहन अध्ययन की इस वैज्ञानिक तकनीक से ज्यादा सटीक परिणाम आने की संभावना रहती है । ठीक गिनती से बाघ संरक्षण की तकनीक उसमें किए जाने वाले निवेश और अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रशिक्षण आदि में मदद मिलती है । दुनिया के पहले बाघ विशेषज्ञ जार्ज शेलर १९६३ में अमेरिका से भारत आए थे और उन्होंने डा. कारंथ को सौ साल पुरानी वाईल्ड लाइफ कंजरवेशन सोसायटी (न्यूयार्क) का प्रतिनिधि बनाया था । उनकी संस्था आजकल वन्य प्राणियों के संरक्षण और शोध में लगी है। वर्ष १९९५ में कान्हा और पेंच टाइगर रिजर्वोंा में पहली बार कैमरा ट्रेप के जरिए बाघों की गणना करने के अनुभव के बारे में डॉ. कारंथ ने बताया कि तब कान्हा में सौ वर्ग किलोमीटर में १२ और पेंच के इतने ही इलाके में चार बाघ पाए गए थे। बाघ के शिकार हिरण, चीतल गौर और सांभर जैसे जानवरो की संख्या और माहौल देखकर लगता है कि कान्हा में आज भी स्थिति बदली नहीं है । एक बाघ को आसपास के ५०० में से सालाना ५० जानवरों की जरूरत होती है । डा. कारंथ ने कहा कि नमूना तकनीक में तीन स्तरों पर काम किया जाता है । पहले चरण में वन प्रशासन के सबसे छोटे कर्मचारी बीट गार्ड अपने अपने क्षेत्रों में बाघ के रहन-सहन, शिकार आदि की जानकारी एकत्र करते हैं । फिर रिमोट सेंसिंग से इलाके का जायजा लिया जाता है और चरण में कैमरा ट्रेप के जरिए बाघों की आबादी का घनत्व मापा जाता है । इस तकनीक में गलती की संभावनाएं न्यूनतम रहती है । उन्होंने बताया कि देश में १९६६-६७ से बाघों के पंजों के निशानों (पगमार्क) के आधार पर गणना होती थी । इस्तेमाल से गणना करके अपनी रिपोर्ट दी है । इसमें पगमार्क पद्धति से गिनी गई बाघों की आबादी का एक तिहाई कम होना बताया गया है । डा. कारंथ ने कहा कि सुश्री सुनीता नारायण की अध्यक्षता में बने टाईगर टास्क फोर्स ने वैज्ञानिक पद्धति से गणना करने की सिफारिश की है । हालांकि वह इस रिपोर्ट के वन्य प्राणियों व इन्सानों के सहजीवन वाली सिफारिशों से सहमत नहीं है । उन्होंने कहा कि हमें बाघो की तेजी से घटती संख्या का पता चल गया है । ऐसे में उनके संरक्षण के प्रयास तत्काल शुरू करना चाहिए ।
चिड़ियाआें की ११८६ प्रजातियां विलुप्त् होने के कगार परपर
समूची दुनिया में चिड़ियाघरो की ११८६ प्रजातियां विलुप्त् होने के कगार पर है । नवीनतम शोध के अनुसार चिड़िया वर्ग की कुल १२ प्रतिशत अथवा आठ में से एक प्रजाति इसकी चपेट मेंे है । इनमें से १८२ प्रजातियां तो गंभीरतम खतरे की स्थिति में है । यू एन. मिलेनियम इको सिस्टम एसेसमेंट की परियोजना रिपोर्ट के अनुसार २०५० तक जलवायुपरिवर्तन एवं चिड़ियाआें के आवास स्थल उजड़ने से ४०० से ९०० प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में होने की आशंका है और इक्कीसवीं शताब्दी के अंत तक यह सूची लगभग दुगनी हो जाएगी । वर्तमान में चिड़ियाआें की जिन ११८६ प्रजातियों के लुप्त् होने का खतरा है उनमें से ३२१ प्रजातियां अत्यंत जोखिम की स्थिति में है । इसी तरह ६८० असुरक्षित अवस्था में है । इसके अलावा ७२७ प्रजातियों के लिए वैश्विक स्तर पर खतरा बढ़ गया है । चिड़ियाआें की विविधता और गतिशीलता से पर्यावरणीय परिवर्तन का पता लगाया जा सकता है । बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के अनुसार जलवायु संबंधी परिवर्तन का आंकलन और भविष्यवाणी भी संभव है ।
जंगल की आग का पता देगा आईखाना
सघन जंगलों में लगी आग का पता लगाने के लिए नासा ने नया हाईटेक प्लेन तैयार किया है । इसका उपयोग घने जंगलों में छुपे दुश्मनों को खोजने में भी किया जा सकता है । नासा ने इसे `आईखाना'नाम दिया है । नासा के वैज्ञानिक इसे एक तरह का हथियार मान रहे हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अक्टूम्बर २००७ में इस महत्वपूर्ण हथियार का परीक्षण पूरा कर लिया था । अब इसे अमेरिकी वायु सेना में शामिल किया जा रहा है । किसी सुपरसोनिक विमान की तरह नजर आने वाला यह हथियार मानवरहित है और यह जंगलों के ऊपर आकाश मार्ग से नजर रखने का काम करता है । पिछले दिनों सेन डिएगो और दक्षिण कैलिफोर्निया के जंगलो मेंे लगी आग की सूचना सबसे पहले आईखाना ने ही दी थी । थर्मल इन्फ्रारेड इमेज का उपयोग करके यह हादसे की वास्तविक जगह की सूचना देता है । अमेरिकी वन सेवा के स्पेशल प्रोजेक्ट गु्रप लीडर एवरेट हिंकले कहते हैं कि यह उपकरण केवल आग लगने की सूचना भर देता है, हाईटेक फायरफाइटर के रूप में यह कोई उल्लेखनीय काम नहीं करता । हालाँकि सुदूर और घने जंगलो में लगी आग के वास्तविक स्थान का पता लगाना काफी मुश्किल होता है। इसलिए इस लिहाज से आईखाना का उपयोग महत्वपूर्ण साबित होगा । इसकी दूसरी खूबी जंगलों में छुपे दुश्मनों को पता लगाने की भी है । इसलिए यह सेना के लिए बेहद काम की चीज है । आईखाना का मुख्य काम थर्मल इन्फ्रारेड इमेजनरी के जरिए जंगल की आग का करीब से फोटो लेकर सेंट्रल सर्वर पर भेजना है । यह सूचना होमलैंड सिक्यूरिटी विभाग और पेंटागन दोनों के पास जाएगी । इसमें दो हाईटेक सैटेलाइटों में सेंसर लगे हैं जो टेलीस्कोप और कैमरे की मदद से ३० मीटर की रेंज से पिक्चर लेते है । सेंट्रल सर्वर पर सूचना पहुँचते ही बचाव और राहत का काम तेजी से शुरू हो जाता है ।वैज्ञानिकों ने निकाले आर्सेनिक से निपटने के रास्ते आर्सेनिक नामक विषैला रसायन पदार्थ सिंचाई के माध्यम से खाद्य पदार्थोंा में पहुुच रहा है, जिसके सेवन से हजारों लोग कैंसर जैसी बीमारी के शिकार हो रहे हैं । अब राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक शोध के दौरान इस समस्या से निजात दिलाने के रास्ते निकाल लिए हैं । संस्थान के वैज्ञानिकों ने ऐसे जीन का पता लगा लिया है जो सिंचाईर् के बाद आर्सेनिक के स्तर को कम करने के साथ साथ उसे अनाज व सब्जियों में पहुंचने से रोकने में सफल होगा । शोध के दौरान ऐसे जीन की जानकारी मिली जो धान के पौधे में पहुंचने वाले आर्सेनिक को दोबारा वातावरण में उत्सर्जित कर रहा था । वैज्ञानिकों का कहना है कि इस विधि से तैयार बीजों को बोने से आर्सेनिक की मात्रा अनाज तक नहंी पहुंच सकेगी । विशेषज्ञों के अनुसार इस रसायन का मानव शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है । इसके शरीर में जाने से त्वचा, यकृत, फेफड़े संबंधी बीमारियां हो जाती है ।***
९ स्वास्थ्य जगत
१० ज्ञान विज्ञान
देश के राज्यों में सड़को की खस्ता हालत किसी से छुपी नहीं है । इसके लिए अक्सर किसी स्थान हालत किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति और खराब कंस्ट्रक्शन को जिम्मेदारी ठहराया जाता है । लेकिन अब इसका हल खोज लिया गया है । केरल मेंे प्लास्टिक के कचरे से सड़क बनाने का प्रयोग किया गया है । इससे बनी सड़के न सिर्फ टिकाऊ होंगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार साबित होंगी । कोझीकोड स्थित नेशनल ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग एंड रिसर्च सेंटर (एनएटीपीएसी) ने प्रायोगिक तौर पर वतकारा कस्बे में प्लास्टिक के कचरे से ४०० मीटर सड़क तैयार की है । हालांकि यह प्रयोग पड़ोसी राज्यों तमिलानांडु समेत कुछ अन्य राज्यों में पहले ही किया जा चुका है, लेकिन केरल की पर्यावरणीय और मिट्टी की भिन्नता कारण यह प्रयोग सफल नहीं हो सका था । इस पर रिसर्च सेंटर के शौधकर्ताआें ने दोबारा काम शुरू किया और माना जा रहा है कि अब यह प्रयोग सफल हो गया है । केरल मेंे प्लास्टिक का कचरा बहुतायत मेंे निकलता है, जिसके निपटान की पूरी व्यवस्था नहीं होने से यह पर्यावरण के लिए बेहद नूकसानदायक साबित हो रहा है । सड़क निर्माण में कचरे का उपयोग हो जाने से पर्यावरण संरक्षरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया जा सकेगा और साथ ही सस्ती व टिकाऊ सड़क बनाना आसान हो जाएगा । एनएटीपीएसी के कोऑर्डिनेटर एन विजयकुमार कहते हैं कि थिरूवनंतरपुरम की हाइवे इंजीनियरिंग लैब में डेढ़ साल तक प्लास्टिक के कचरे से सड़क निर्माण के फार्मूले पर परीक्षण किया गया और अब प्रायोगिक तौर पर सड़क बना भी ली गई है । उम्मीद है प्रयोग सफल रहेगा ।वे कहते हैं कि केरल की जलवायु और मिट्टी में काफी भिन्नता होने के कारण एक फार्मूले को सभी जगह अमल में लाना संभव नहीं था, लेकिन अब सभी जगह के लिए यह प्रयोग सफलतापूर्वक कर लिया गया है । श्री विजयकुमार का कहना है कि प्लास्टिक के कचरे से सड़क बनाने पर १० प्रतिशत तक डामर की बचत होगी । एकटन प्लास्टिक कचरे से साढ़े तीन मीटर चौड़ी एक किलोमीटर सड़क बनाई जा सकती है । इसमेंे खर्चा भी पारंपरिक डामर की सड़कों की तुलना में काफी कम आता है । इस प्रक्रिया मेंे प्लास्टिक के टुकड़ों को पिघलाकर गिट्टी के साथ मिलाया जाता है । इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि तापमान १६० से १७० डिग्री सेल्सियस के बीच ही होना चाहिए वरना मिश्रण के चिपकने की क्षमता प्रभावित होती है । केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल भी इस तकनीक को पर्यावरण हितैषी घोषित कर चुका है
करियर और वेतन के लिहाज के आकर्षक माने जाने वाले बीपीओ, आईआी और इलेक्ट्रोनिक मीडिया जैसे नए क्षेत्र स्वास्थ्य के लिहाज से खतरनाक साबित हो रहे हैं । लेकिन अब इन चमकते उद्योगों के काले पहलू भी सामने आने लगे है । इन उद्योगो में कार्य के घंटे लंबे होते हैं, रात की शिफ्त लंबी अवधि तक चलती है , लक्ष्य कठिन होते हैं, अपनी होते हैं, अपनी पहचान स्थपित करने की कड़ी प्रतिस्पर्धा और नौकरी पर हमेशा असुरक्षा के बादल मँडराते रहते हैं । ये सभी पहलू यहाँ काम करने वालों को दिल के दौरे, हृदय रोग, पाचन की गड़बड़ियाँ, मोटापा, डिपे्रशन, तनाव, अनिद्र और जोड़ो में दर्द शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक सामस्याआें के शिकार बना रहे हैं । एक अनुमान के अनुसार बीपीओ उद्योग में १६ लाख युवा कार्यरत है । करीब इतने ही लोग आईटी एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया में काम कर रहे हैं । विशषज्ञों का कहना है कि इन उद्योगों में काम करने वाले युवाआें की स्थूल जीवन शैली, काम की लंबी अवधि, तनावपूर्ण कार्य स्थितियाँ और तीव्र प्रतिस्पर्धा के कारण इनमें उम्र में ही गंभीर बीमारियाँ पैदा हो रही है । मेट्रो हॉस्पिटल एवं हार्ट इंस्टीट्यूट के निदेशक हृदय रोग विशषज्ञ डॉ. पुरुषोत्तम लाल ने बताया कि लंबे समय तक तनाव में रहने अथवा लंबे समय तक विपरीत एंव तनावपूर्ण कार्य स्थितियों मेंकार्य करने के कारण रक्तचाप ब़़ढने, हृदय की रक्त नलियों में रक्त के थक्के बनने और दिल के दौरे पड़ने के खतरे बढ़ जाते है। उन्होने कहा कि पिछले कुछ वर्षो में पेशेगत कार्यो से संबंधित तनाव, काय्र के घंटे बढ़ने और गलत-गलत रहन-सहन एवं खान-पान, धुम्रपान फास्ट फूड और व्यायाम नहीं करने जैसे कारणों से युवाआें में दिल के दोरे एंव हृदय रोगों का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है । ***
११ कविता
वृक्ष बोलते हैं
प्रेम वल्लभ पुरोहित
`राही' वृक्ष बोेलते हैं
इतिहास रचा है इन्हांने ।
माँ कहती-कहती थक गयी
कि जन्म से मरण तक का
साथ रहा है
रहता है
मनुष्य से इनका ।
नाता ऐसा जुड़ा है
फिर भी नातेदार
थमाली कुल्हाड़ी से काटता है इन्हें
जन्म से आजीवन तक की सेवा
क्या-क्या कहें
अपने मुख से अपनी बड़ाई
अच्छी लगती नहीं
मृत्यु के दिन भी
घाट तक की यात्रा मेंे साथ रहते हैं
वृक्ष (लकड़िया)
यही नहीं -
पंचतात्विक शरीर को
भस्मकर मुक्ति देते हैं
स्वर्ग देते हैं ये वृक्ष
ऐसा नाता
जीवन मरण तक
साथ निभाता है जो विस्मयकारी है ।
मानव,
धरती माता को नग्न न रहने दो
लहलहाते हरित वृक्षों से करते श्रृंगार
धरती माता का ।***