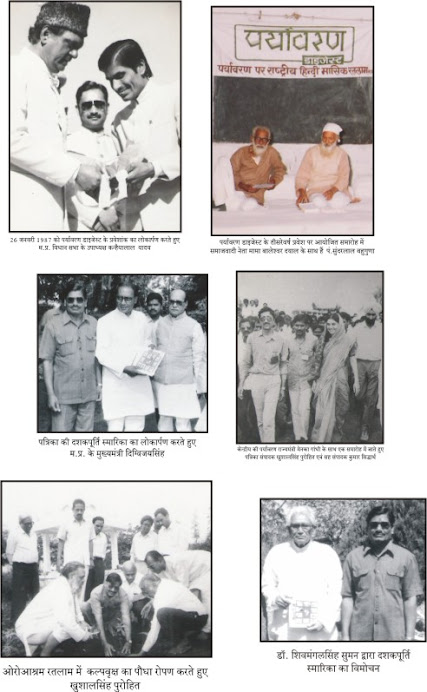सोमवार, 20 मई 2019
सम्पादकीय
गोंद के लिए पेड़ों को रसायन के इंजेक्शन
मध्यप्रदेश मेंसतपुड़ा के जंगलों में इन दिनों गोंद माफिया सक्रिय है । धावड़ा और सलाई के पेड़ों में अप्राकृतिक तरीके से रासायनिक इंजेक्शन लगाकर गोंद निकाला जा रहा है । इस प्रक्रिया में माफिया जंगल से जूड़े आदिवासियों का उपयोग कर रहे हैं । रासायनिक इंजेक्शन लगाने से इन पेड़ों को जहां पर्यावरणीय नुकसान हो रहा है, वहीं पेड़ निर्धारित क्षमता से अधिक गोंद उगल रहे हैं । यह गोंद सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है । इन पेड़ों की पत्तियों के सेवन से मवेशियोंको भी खतरा बना हुआ है । गोंद के कारोबार में क्षेत्रीय कारोबारियों के अलावा अन्य स्थानों के लोग भी आने लगे हैं और यह सबकुछ प्रतिबंध के बाद हो रहा है । जिम्मेदार अधिकारी इस गोरखधंधे की बात को नकार रहे है ।
सूत्र बताते है कि महाराष्ट्र सीमावर्तीसतपुड़ा पर्वत के वनक्षेत्रों से लगे बड़वानी जिले के बरला, बलवाड़ी और खरगौन जिले के महादेव सिरवेल से लेकर सुलाबेडी सहित बुरहानपुर के असीरगढ़ तक फैले वन क्षेत्रों में गोद निकाला जा रहा है । यह लगभग ६०-७० किमी का लम्बा इलाका है । जंगलों में २०० से अधिक श्रमिक को इस काम में लगाया गया है । केमिकल की मदद से निकलने वाला गोंद सामान्य गोंद से अधिक चमकदार होता है । यह गोद किराना दुकानों के अलावा थोक व्यापारियों को भी बेचा जा रहा है ।
इंजेक्शन से गोद निकालने से वन और पर्यावरण को खतरा पहुंचता है । महाराष्ट्र में इसको लेकर अन्य नियम होने की वजह से तस्करी रोकने में दिक्कत आती है ।
इथिफोन रसायन के उपयोग से गोंद निकालने की कोशिश में ५-६ साल में वृक्ष नष्ट होने लगते है । यह प्रक्रिया असंवहनीय एवं अप्राकृतिक है, इसलिए हो रही क्षति को रोकने के लिए एक जनवरी २०१९ से गोंद निकालने पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया है ।लेकिन सवाल यह है कि प्रतिबंध केबावजूद यह सिलसिला जारी है जो प्रकृति के साथ ही मानव जीवन के लिए भी खतरा है ।
प्रसंगवश
उत्तरप्रदेश में महाभारत काल के अवशेष मिले
महाभारत काल में इसानों की वेश-भूषा कैसी रही होगी ? टीवी के पात्रोंऔर किताबों में पढ़कर महाभारत काल को लेकर हमारी समझ कितनी सही है ?
उ.प्र. में बागपत के सिनौली में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई)द्वारा कराई जा रही खुदाई से आने वाले सालों में इससे पर्दा उठ सकता है ? खुदाई से शाही शव पेटिकाएं, रथ, कंकाल, आभूषण समेत कई ऐसी चीजे मिली हैं, जिन्हें महाभारत काल से जोडकर देखा जा रहा है ।
इस बार खुदाई में एक चैम्बर व दो और शव पेटिकाएं मिली हैं । इनमें जली लकड़ी के अवशेषों से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस चैम्बर को मृत देह को स्नान कराने व पूजा-पाठ के लिए उपयोग में लाया जाता होगा । पुरातत्वविद सीधे तौर पर इसे महाभारत काल के समय की संस्कृति कहने से बच रहे हैं लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि यह हड़प्पा सभ्यता नहीं है ।
हड़प्पा के समानांतर या इससे पहले की संस्कृति है । पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत के सिनौली में अभी तक तीन बार खुदाई हो चुकी है । सबसे पहले वर्ष २००५-०६ में खुदाई हुई थी । इसके बाद वर्ष २०१८ में और फिर इस साल जनवरी में खुदाई का कार्य शुरू हुआ था ।
हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से ताम्र सामान आदि की आकृति एक-दूसरे से अलग है । ताम्र हथियार बनाने की प्रक्रिया और उनके आकार हड़प्पा सभ्यता की किसी भी खुदाई में मिले साक्ष्यों से नहीं मिलते है । यहां मिले मनके आदि हड़प्पा तकनीक से अलग है ।
हड़प्पा सभ्यता के लिए अभी तक ५०० स्थानों पर खुदाई हो चुकी है, लेकिन शवधान में चार पाये वाली शव पेटिकाएं, रथ व युद्ध के समय उपयोग में लाए जाने वाले हथियार आदि किसी अन्य स्थान पर नहीं मिल हैं ।
सवाल यह है कि हमारा देश इतना विशाल है और यहां क्या केवल एक ही संस्कृति के लोग रहते रहे होंगे । एक ही संस्कृति विकसित रही होगी, ऐसा कैसे हो सकता है । साक्ष्योंके आधार पर मात्र कहा जा रहा है कि यह हड़प्पा सभ्यता नहीं है । यहां मिलेसाक्ष्य हड़प्पा की संस्कृति से बिल्कुल मेल नहीं खाते है । यह संस्कृति यमुना और गंगा के बीच के इलाके में पुष्पित और पल्लवित हो रही थी ।
सामयिक
चुनाव में ओझल है पर्यावरण के मुद्दे
डॉ. ओ.पी. जोशी
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सर्वोच्च् सदन लोकसभा केचुनाव चल रहे है, परन्तु चुनावी अभियान से लोक-जीवन के जल, जंगल एवं जमीन के मुद्दे गायब हैं ।
सब जानते हैं कि देश का आर्थिक विकास एवं 'सकल घरेलू उत्पाद` (जीडीपी) इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर रहता है । भारत जैसे कृषि-प्रधान देश में तो ये संसाधन पैदावार बढ़ाने हेतु भी जरूरी हैं । 'विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग` की १९८७ में जारी रिपोर्ट में बड़ी दृढ़ता एवं स्पष्टता से कहा गया था कि ``सभी देशों की सरकारें यह समझ लें कि उनके देश की अर्थव्यवस्था जिस नाजुक धुरी पर टिकी है, वह है-वहां के प्राकृतिक संसाधन,`` लेकिन मौजूदा चुनाव अभियान बताते हैं कि हमारे देश में जल, जंगल एवं जमीन की कोई पूछ-परख नहीं है ।
मसलन, जीवन का आधार माने गये जल की उपलब्धता लगातार घटती जा रही है । आजादी के समय प्रति व्यक्ति ६००० घन मीटर (घ.मी.) जल उपलब्ध था जो वर्ष २०१० में घटकर लगभग १६०० घ.मी. ही रह गया । 'केन्द्रीय जल-संसाधन मंत्रालय` के अनुसार यह जल उपलब्धता वर्ष २०२५ में १३४१ घ.मी. तथा २०५० तक ११४० घ.मी. ही रह जावेगी । 'वर्ल्ड-रिसोर्स इंस्टीट््यूट` की मार्च, २०१६ की रिपोर्ट के अनुसार भारत का ५४ प्रतिशत हिस्सा पानी की कमी से परेशान है।
'नीति आयोग` की २०१८ की रिपोर्ट में भी बताया गया है कि एक तरफ, देश के लगभग ६० करोड़ लोग पानी की भयानक कमी से जूझ रहे हैं तो दूसरी तरफ, ७० प्रतिशत पानी पीने योग्य नहीं बचा है। भू-जल स्तर गिरने, सूखा, कृषि, कारखानों एवं निर्माण कार्यांे में बढ़ती पानी की मांग, सतही जल-स्त्रोतों के बढ़ते प्रदूषण एवं गलत जल प्रबंधन जैसी चुनौतियां, मौसमी बदलाव व जलवायु परिवर्तन के चलते और बढ़ेंगी ।
जल एवं जंगल के अटूट रिश्ते को कौन नहीं जानता ? किसी प्रकृति प्रेमी ने वर्षों पूर्व लिखा था कि ``जिन पेड़ों, जंगलों पर बादलों के जनवासे (बारात के ठहरने की जगह) दिए जाते थे, उनका सफाया हो रहा है । 'राष्ट्रीय वन नीति` के अनुसार मैदानी तथा पहाड़ी क्षेत्रों में क्रमश: ३३ एवं ६६ प्रतिशत भू-भाग पर जंगल होना जरूरी है, परंतु यह स्थिति कहीं ठीक नहीं है। आज देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग २१-२२ प्रतिशत पर ही जंगल है । इनमें भी २-३ प्रतिशत सघन वन, ११-१२ प्रतिशत मध्यम वन और ९-१० प्रतिशत छितरे जंगल हैं । देश के १६ पहाड़ी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में केवल ४० प्रतिशत भाग पर ही जंगल है ।
उत्तर-पूर्वी राज्यों में देश के जंगलों का एक चौथाई हिस्सा है, परंतु यहां वर्ष २०१५ से २०१७ के मध्य लगभग ६३० वर्ग किमी जंगल क्षेत्र घट गया है। यह इलाका दुनिया के १८ प्रमुख जैव-विविधता क्षेत्रों (हाट स्पॉट्स) में आता है। जानकारों के अनुसार लगभग ८० प्रतिशत जैव-विविधता जंगलों में ही पायी जाती है। एक आंकलन के अनुसार देश में जंगलों के घटने से २० प्रतिशत से ज्यादा जंगली पौधों एव जीवों पर विलुप्ति का खतरा फैल गया है । हिमालयी पर्वतमाला, अरावली पहाडियां, विंध्याचल एवं सतपुड़ा के पहाड़ तथा पश्चिमी-घाट क्षेत्र में भी विकास कार्यो हेतु भारी मात्रा में जंगल काटे गये हैं एवं काटे जा रहे हैं । बीसवीं सदी के अंत तक अरावली पहाडियों पर ५० प्रतिशत हरियाली थी जो अब घटकर महज .०७ प्रतिशत रह गयी है। अवैध, खनन सेेकई स्थानों पर समाप्त पहाडियों के कारण थार के रेगिस्तान की रेत दिल्ली की ओर आ रही है । जाहिर है, देश की राजधानी दिल्ली रेगिस्तान विस्तार की गिरफ्त में है ।
जल एवं जंगल का जमीन से भी गहरा रिश्ता होता है, क्योंकि जमीन ही इन दोनों को जगह देकर खेती में भी मद्दगार होती है। खेती के लिए उपजाऊ भूमि जरूरी है, परन्तु हमारे देश में खेती की भूमि पर दो प्रकार के संकट हैं । पहला, बढ़ते शहरीकरण, औद्योगी-करण एवं परिवहन योजनाओं के कारण इसका क्षेत्र घटता जा रहा है। दूसरा, बाढ़, सूखा, अम्लीयता, क्षारीयता, प्रदूषण एवं जल-जमाव आदि कारणों से इसकी उत्पादकता कम हो रही है।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने कुछ वर्ष पूर्व अपने एक अध्ययन में बताया था कि देश की कुल १५० करोड़ हेक्टर कृषि भूमि में से लगभग १२ करोड़ की पैदावार घट गयी है एवं ८४ लाख हेक्टर समस्या ग्रस्त है। आठ राज्यों (राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड एवं त्रिपुरा) में लगभग ४० से ७० प्रतिशत भूमि कई कारणों से बंजर होने की कगार पर है ।
कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि देश में जल, जंगल, जमीन एवं खेती के हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन इन पर किसी भी राजनैतिक दल ने सत्रहवीं लोकसभा के इस चुनाव में कोई गंभीरता नहीं दिखाई है। किसानों को कर्जमाफी एवं कुछ कुछ राशि देने की ही चर्चाएं होती रहीं हैं, परंतु इससे जल, जंगल, जमीन एवं खेती के सुधरने के कोई आसार नजर नहीं आते । ये सारे संसाधन मनुष्य के जीवन-व्यापन हेतु जरूरी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ती करते हैं । यह मनुष्य ही आखिरकार चुनाव में भी वोटर या मतदाता होता है।
राजनैतिक दल इन संसाधनों के रख-रखाव, संरक्षण एवं उन्हें बढ़ाने की ओर प्रतिबद्धता दर्शाते तो यह वोटरों को लाभ पहुंचाने का ही प्रयास माना जाता। देश में जलवायु परिवर्तन से पैदा समस्याओं के प्रति भी विभिन्न राजनीतिक दलों ने उदासीनता ही दिखायी है । कई देशों में तो अब पर्यावरण संरक्षण हेतु अलग से दल तक बन रहे हैं, परंतु हमारे यहां अभी तक किसी भी लोकसभा चुनाव में पर्यावरण, कोई मुद्दा तक नहीं बना है ।
हमारा भूमण्डल
हम व्यापक जैव विलुिप्त् की कगार पर हैं
सोमेन्द्र सिंह खरोला
जैव मंडल की तुलना एक बहुत बड़ी दीवार से की जा सकती है, मनुष्य जिसके ऊपर बैठा है। अगर इस जैव मंडल में से हम जानवरों की कुछ प्रजातियां गंवा भी देते हैं,तो दीवार से महज कुछ इंर्टें गुम होंगी, दीवार तो फिर भी खड़ी रहेगी। परंतु यदि अधिकाधिक जानवर विलुप्त् होते जाएंगे, तो पूरी दीवार भी दरक सकती है। सवाल है कि इंर्टों को हटा कौन रहा है?
व्यापक जैविक विलोपन ऐसी वैश्वक घटना को कहते हैं जिसके दौरान पृथ्वी के ७५ प्रतिशत से अधिक वन्य जीव विलुप्त् हो जाते हैं । पिछले ५० करोड़ वर्षों में, इस तरह के व्यापक विलोपन की पांच घटनाएं हुई हैं। इनमें से सबसे हालिया विलोपन ने डायनासौर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। लेकिन कितने लोग यह जानते हैंकि हाल ही में किए गए कई शोध अध्ययनों ने समय-समय पर यह दावा किया है कि पृथ्वी एक और व्यापक विलोपन घटना की गिरफ्त में है: छठा व्यापक विलोपन ।
दरअसल, पिछले १०० वर्षों में, रीढ़धारी प्राणियों की २०० प्रजातियां विलुप्त् हो चुकी हैं। प्रजातियों के विलुप्त् होने की यह दर (प्रति वर्ष २ प्रजातियां), आपको शायद मामूली लगे और शायद चिंता का विषय भी न हो। शायद आप कहें कि जीव तो हर समय विलुप्त् होते रहते हैं, यह तो प्रकृति का तरीका है। लेकिन पिछले बीस लाख वर्षों में विलोपन की दर को देखें तो २०० प्रजातियों को विलुप्त् होने में सौ नहीं बल्कि दस हजार साल लगना चाहिए थे। दूसरे शब्दों में, विलुप्त् होने की दर पहले के युगों की तुलना में पिछले मात्र १०० वर्षों में लगभग १०० गुना बढ़ गई है।
प्रोसीडिंग्स ऑफ दी नेशनल एकेडमी ऑफसाइंसेज जर्नल में हाल ही में प्रकाशित एक शोध आलेख छठे व्यापक विलोपन के अपने दावों के साथ एक कदम और आगे बढ़ता है।
यह अध्ययन बताता है कि न केवल छठा व्यापक विलोपन एक वास्तविकता है, बल्कि इसके परिणाम हमारे सोच से कहीं अधिक गंभीर होंगे। इसके अलावा यह अध्ययन इसके लिए पूरी तरह मनुष्यों को जिम्मेदार ठहराता है। यह काफी दिलचस्प बात है कि पहला व्यापक विलोपन, जो मनुष्य के अस्तित्व में आने से बहुत पहले हुआ था, वह भी उल्काआें की बौछार या ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण नहीं बल्कि जीवों के द्वारा ही हुआ था।
अपने शोध पत्र में लेखक - गेरार्डो सेबालोस, पॉल आर. एह्यलिच, रोडोल्फो दिर्जोलिखते हैं कि पिछले कुछ दशकों में, प्राकृतवासों की हानि, अतिदोहन, घुसपैठी जीव, प्रदूषण, विषाक्तता, और हाल ही में जलवायु की गड़बड़ी, तथा इन कारकों के बीच परस्पर क्रियाएं आम एवं दुर्लभ कशेरुकी आबादियों की संख्या और उनके आकार दोनों में भयावह गिरावट का कारण बनी है। इसके अलावा, अध्ययन के अनुसार, पिछले सौ वर्षों में, हमारे साथ पृथ्वी पर रहने वाले रीढ़धारी जीवों की ५० प्रतिशत संख्या खत्म हो चुकी है, और इस तरह से जीवों की आबादी का ऐसा भयावह पतन इस ओर संकेत देता है कि छठा व्यापक विलोपन शुरू हो चुका है । लेकिन इस व्यापक विलोपन के कारण यदि ७५ प्रतिशत से अधिक जीव भी खत्म हो जाएं मनुष्य होने के नाते हम क्योंपरवाह करें? क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न जीव एक दूसरे पर निर्भर हैं, श्रृंखला प्रभाव की तरह मनुष्यों पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।
उदाहरण के लिए कीट-पतंगों को ही लीजिए । पर्यावरण कीटों की अनुपस्थिति के अनुकूल हो पाए यदि उससे पहले ही कीटों की हजारों प्रजातियां विलुप्त् हो जाएं, तो पेड़ों की हजारों प्रजातियां भी गायब हो जाएंगी, क्योंकि पेड़ों की कई प्रजातियां परागण के लिए कीटों पर निर्भर होती हैं । अगर पेड़ गायब हो जाते हैं, तो मानव जाति के लिए यह मौत की दस्तक होगी। हमारी धरती की हवा गंदी और जहरीली तो होगी ही, पृथ्वी का तापमान कई डिग्री बढ़ जाएगा। भू-क्षरण की दर बढ़ेगी जिससे कृषि योग्य भूमि का नुकसान होगा। वर्षा गंभीर रूप से प्रभावित होगी, जिसके फलस्वरूप मीठे पानी के स्त्रोतों की गुणवत्ता के स्त्रोतों की गुणवत्ता पर भी असर होगा। निश्चित रूप से, मानव पर नकारात्मक वार होगा ।
यह देखते हुए कि यह बड़े पैमाने का विलोपन मानव अस्तित्व के लिए एक वास्तविक खतरा साबित हो सकता है, यह काफी निराशा-जनक है कि इस विलोपन के प्राथमिक कारण - यानी हम - इससे बेखबर हैं। इसकी ओर ध्यान न देने के दो कारण हैं ।
पहला कारण है, औसतन हर साल गायब होने वाली दो प्रजातियां ऐसी होती हैं जो या तो हमारे लिए आकर्षक नहीं हैं (शेर की तरह आकर्षक नहीं हैं) या दुनिया के अलग-थलग कोनों में रहती हैं, इसलिए हम उस नुकसान को महसूस नहीं करते हैं।
विलोपन के खतरे की सूचना से हमें अनभिज्ञ रखने वाला दूसरा कारण यह है कि पृथ्वी के वन्य जीवन के स्वास्थ्य का आकलन करने हेतु शोध अध्ययनों का पूरा ध्यान केवल अंतिम बिन्दु पर रहा है - यानी जीवों की प्रजातियों का पूरी तरह विलुप्त् हो जाना। और वर्तमान अध्ययन यही बताता है कि अंतिम बिन्दु आधारित उन अध्ययनों ने व्यापक विलोपन के परिमाण को कम करके आंका है। अगले हिस्से में इस बात को विस्तार में स्पष्ट किया गया है।
तर्क को आगे बढ़ाने के लिए, एक जीव प्रजाति द पर विचार करते हैं। यह जीव द एशिया के पंद्रह अलग-अलग देशों में फैला हुआ है। दूसरे शब्दों में इस जीव की वैश्विक आबादी पंद्रह अलग-अलग देशों में फैली हुई स्थानीय आबादियों से मिलकर बनी है। किसी भी देश में, इस जीव की स्थानीय आबादी में एक निश्चित संख्या में जीव होंगे; किसी अन्य देश में एक निश्चित संख्या की स्थानीय आबादी होगी, और इसी तरह सब देशों में अलग अलग स्थानीय आबादियां होंगी।
मान लीजिए, एक साल के बाद, पंद्रह स्थानीय आबादियों में से चौदह खत्म हो जाती हैं और केवल एक अंतिम स्थानीय आबादी बची रह जाती है।
ऐसे परिदृश्य में, अगर हम केवल अंतिम बिन्दु - यानी इस जीव प्रजाति का पूर्ण विलोपन - पर ध्यान केन्द्रित करेंगे, तो हर साल हम जीव द के सामने एक टिक मार्क लगाकर इसे विलुप्त् नहीं की श्रेणी में डाल देंगे क्योंकि एक स्थानीय आबादी तो बची हुई है ।
विलुप्त् या विलुप्त् नहीं का यह सख्त विभाजन जंगल में उपस्थित किसी प्रजाति के वास्तविक स्वास्थ्य को समझने का एक अपरिष्कृत तरीका है। इस मामले में, उदाहरण के लिए, केवल जीव द को विलुप्त् नहीं के रूप में अंकित करके, हम जीव द की सोचनीय स्थिति जैसी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त् करने में विफल हो जाते हैं । इसकी स्थानीय आबादियों की संख्या में भारी गिरावट आई है। इस काल्पनिक परिदृश्य में यह संख्या १५ से घटकर एक तक आ पहुंची है। अर्थात व्यापक विलोपन को कम करके आंका जा रहा है ।
इसलिए, वर्तमान अध्ययन के अनुसार, वर्तमान व्यापक विलोपन की घटना का सही अनुमान लगाने के लिए, यह जरूरी है कि प्रजातियों की स्थानीय आबादियों के विलुप्त् होने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाए, न कि केवल वैश्विक विलुिप्त् पर । कोई जीव जीवित है इसका मतलब यह नहीं कि वह फल-फूल रहा है ।
पिछले सभी अध्ययनों में इसी दोषपूर्ण रास्ते को अपनाया गया है जिनमें केवल अंतिम बिन्दु पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। इस प्रकार ये अध्ययन इस गलतफहमी के शिकार हैं कि जैव विविधता के नुकसान का दौर शुरू ही हो रहा है, और मानव जाति के पास इसका मुकाबला करने के लिए कई दशकों का समय उपलब्ध है। विलुप्त् होने की दर केवल दो जीव प्रति वर्ष ही तो है। लेकिन वर्तमान अध्ययन इसका जोरदार विरोध करता है: हम इस बात पर जोर देते हैं कि छठा सामूहिक विलोपन शुरू हो चुका है और प्रभावी कार्रवाई के लिए वक्त बहुत कम है, शायद दो या तीन दशक । शायद, इससे भी कम ।
बेशक, यह कहना सही नहीं है कि मानव जाति कुछ दशकों के भीतर विलुप्त् हो जाएगी; लेकिन अगर हमने अभी कार्य करना शुरू नहीं किया तो यह व्यापक विलोपन दो या तीन दशकों के भीतर अपरिवर्तनीय साबित होगा। नतीजतन, इसके साथ ही मानव जाति के विलोपन की संभावना शुरू हो जाएगी ।
इस तरह के मजबूत दावे का समर्थन करने के लिए, यह अध्ययन एक नए दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। पूर्व अध्ययनों के विपरीत, यह दो महत्वपूर्ण कारकों को ध्यान में रखता है जो अंतिम बिन्दु - अर्थात किसी जीव प्रजाति के संपूर्ण वैश्विक विलोपन - से ठीक पहले सामने आते हैं । पहला है, जैसा कि ऊपर कहा गया, पिछले सौ वर्षों में विभिन्न जीव प्रजातियों की स्थानीय आबादियों में कमी । दूसरा है, इसी अवधि में उनके भौगोलिक आवास में कमी। (नोट : इस अध्ययन के लिए, २७,६०० कशेरूकी जीवों की स्थानीय आबादियों पर ध्यान दिया गया, जो दुनिया की कुल लगभग ८७ लाख जीव प्रजातियों का एक छोटा-सा अंश है।)
अध्ययन बताता है कि पिछले सौ वर्षों में विभिन्न जानवरों की एक अरब स्थानीय आबादियां विलुप्त् हो चुकी हैं । जी हां, एक अरब । इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया में एक अरब जीव प्रजातियां विश्व स्तर पर पूरी तरह से विलुप्त् हो चुकी हैं, बल्कि यह है कि विभिन्न प्रजातियों की कुल एक अरब स्थानीय आबादियां दुनिया के कुछ क्षेत्रों में हमेशा के लिए खत्म हो गई है, जबकि ये जीव अभी भी दुनिया के अन्य क्षेत्रों में मौजूद है। अर्थात, इन प्रजातियों का स्थानीय विलोपन हुआ है।
उदाहरण के लिए, एक समय में एशियाई शेर की हजारों स्थानीय आबादियां पूरे भारत में पाई जाती थी। लेकिन समय के साथ, ये सभी स्थानीय आबादियां, अन्य जीवों की एक अरब स्थानीय आबादियों के साथ विलुप्त् हो गइंर् । आज, एशियाई शेरों की अंतिम कुछेक स्थानीय आबादियां गुजरात में एक अलग-थलग भाग (गिर वन) में पाई जाती है। जब ये चंद अंतिम स्थानीय आबादियां विलुप्त् हो जाएंगी, तो एशियाई शेर को विश्व स्तर पर विलुप्त् कर दिया जाएगा। तब यह विश्व में कहीं भी नहीं पाया जाएगा ।
अध्ययन एक और विचलित करने वाला तथ्य बताता है। पिछले सौ वर्षों में, पृथ्वी की रीढ़धारी प्रजातियों में से ३२ प्रतिशत की आबादी के आकार और भौगोलिक विस्तार में कमी आई है। अध्ययन में विश्लेषण किए गए सभी १७७ स्तनधारियों ने अपने भौगोलिक क्षेत्रों का ३० प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सा खो दिया है। और ४० प्रतिशत से अधिक प्रजातियों की सीमा ८० प्रतिशत से अधिक घट गई है। और तो और, जीवों की जिन प्रजातियां को कम चिंता की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, वे भी इसी तरह के संकटों से पीड़ित हैं और लगातार लुप्त्प्राय श्रेणी की ओर बढ़ रही हैं ।
हमारा डैटा बताता है कि प्रजातियों के विलुप्त् होने से परे, पृथ्वी स्थानीय आबादियों में गिरावट और विलुप्त् होने की एक विशाल घटना का सामना कर रही है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य और सेवाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा । यह पारिस्थितिकी तंत्र सभ्यता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। अंतत: मानवता इस ब्राह्मण्ड में जीवन के एक मात्र समुच्च्य के उन्मूलन की बहुत बड़ी कीमत चुकाएगी ।
इसलिए, भले ही विश्व स्तर पर हर साल मात्र दो प्रजातियां विलुप्त् हो रही हों, यह मात्र दो की संख्या दुनिया भर में विभिन्न जीव प्रजातियों की सैकड़ों-हजारों स्थानीय आबादियों के कठोर और व्यापक विलोप का संकेत देती है। आखिरकार, इस तरह स्थानीय आबादियों और प्राकृतवासों का नुकसान कुछ ही समय में हजारों जीव प्रजातियों के वैश्विक विलोप का कारण बन जाएगा: जिसको व्यापक विलोपन कहते हैं ।
तो, हम स्थानीय आबादियों के विलोपन की इस लहर का मुकाबला कैसे करें और छठे सामूहिक विलोपन को कैसे रोकें ?
इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए चाहें तो वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रमों, लोक निकायों, राष्ट्रीय नीतियों, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी वगैरह की बात कर सकते हैं। लेकिन इस सवाल का असली जवाब वह है जो हम - और हाई स्कूल का कोई भी छात्र - लंबे समय से जानते हैं। यह एक ऐसा जवाब है जिसे इतनी बार दोहराया गया है कि ऐसा लगता है कि इसकी धार बोथरी हो गई है: उपभोग में कमी करें, जनसंख्या पर लगाम कसें ।
हालांकि, अध्ययन के नापसंद दावों को देखते हुए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कई वैज्ञानिकों ने इसके निष्कर्षों पर सवाल उठाए हैं ।
इन वैज्ञानिकों को लगता है कि यह अध्ययन फालतू में भेड़िया आया, भेड़िया आया का शोर मचाने जैसा है, क्योंकि व्यापक विलुिप्त् की घटनाओं के इरादे कहीं अधिक सख्त होते हैं । इन शंकालुओं का मानना है कि व्यापक विलुिप्त् की घटनाएं लाखों वर्षों में सामने आती हैं । इसलिए यह मान लेना जल्दबाजी होगी कि पानी सिर से ऊपर जा चुका है । आखिरकार इस अध्ययन में मात्र पिछले १०० वर्षों में केवलरीढ़धारी जीवों की विलुिप्त् की संख्या पर ही तो विचार किया गया है । यह अवधि पिछले बड़े पैमाने पर विलोपन घटनाओं की तुलना में पलक झपकाने जैसी है। कीटों और अन्य गैर-कशेरुकी जीवों का क्या ? केवल २७,६०० कशेरुकी जीवों पर ध्यान केन्द्रित करके (जो कुल ८७ लाख जीव प्रजातियों का अंश-मात्र है) यह अध्ययन व्यापक विलुिप्त् की घटना की एक ऐसी तस्वीर खींचता है जो वास्तविकता से कहीं अधिक गंभीर और अतिरंजित बन गई है।
इसके अलावा, एक यह तर्क भी दिया जा सकता है कि विलोपन के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए मनुष्य नामक प्राणि कोई न कोई समाधान खोज निकालेगा । जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यह ध्यान रखना समझदारी होगी कि जैविक व्यापक विलोपन की घटना अचानक होने वाली घटना नहीं है जो पूरी मानव जाति को एक झपट्टा मारकर समाप्त् कर देगी। यह सही है कि ऐसी घटना केदौरान अल्पावधि में हजारों जीव प्रजातियां उच्च् दर से विलुप्त् हो जाती हैं, लेकिन यह अल्पावधि लाखों वर्षों में फैली होती है। यह लम्बी अल्पावधि मनुष्य को पेड़ों में परागण के लिए रोबोट विकसित करने के लिए पर्याप्त् हो सकती है।
उसी तरह यदि विश्व के मत्स्य भंडार प्रभावित होते हैं, तो यह अल्पावधि कृत्रिम मांस तैयार करने केलिए काफी है। यहां तक कि ऐसी प्रौद्योगिकियों का निर्माण करने के लिए भी यह पर्याप्त् समय हो सकता है, जिससे विलुप्त् पेड़-पौधों की नकल कर वायुमंडलीय ऑक्सीजन और अन्य गैसों की निश्चित मात्रा को बरकरार रखा जा सके । तब तक, हम अन्य ग्रहों पर बस ही चुके होंगे। तो, व्यापक विलोपन का खतरा उतना बुरा नहीं हो सकता है जितना लगता है, कम से कम मनुष्योंके लिए तो नहीं।
फिर भी, यह अध्ययन दावा क्रता है िक् अगर हम अभी, दो या तीन दशकों के अंदर, कार्रवाई नहीं करते हैं तो सामूहिक विलोपन स्थायी होगा। नतीजतन, स्थानीय आबादियों के विलुप्त् होने की दर कैंसर की तरह बढ़ सकती है। इसके परिणामस्वरूप जैव विविधता में गिरावट आएगी और मानव अस्तित्व के लिए खतरा पैदा हो जाएगा।
लेकिन क्या जैव विविधता में गिरावट हमारे तकनीकी विकास को पछाड़ देगी ? खतरे की घंटी बजाने से पहले इस सवाल पर विचार करना जरूरी है । फिर भी, मैं कहना चाहूंगा कि हमने पिछले सौ वर्षों में ५० प्रतिशत कशेरुकी जीवों का सफाया तो कर दिया है, अगर अब कुछ नहीं किया गया तो हम जल्द ही बचे हुए ५० प्रतिशत को भी खो सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से, विलुप्त् होने की गति को देखते हुए, मेरे मन में सवाल आता है कि क्या मानव के पास, प्रौद्योगिकी या अन्य माध्यम से, इसका सामना करने के लिए पर्याप्त् समय होगा । इसके अलावा, जैव विविधता के नुकसान की ऐसी दर पहले हो चुकी विलोपन की घटनाओं से कहीं अधिक विनाशकारी साबित हो सकती है।
मेरे साथ बातचीत के दौरान अध्ययन के प्रमुख लेखक गेरार्डो सेबलोस ने कहा था कि इससे यह और भी जरूरी हो जाता है। पिछले सभी व्यापक विलोपन की घटनाएं लाखों वर्षों में फैली हुई थीं, लेकिन वर्तमान व्यापक विलोपन केवल कुछ सौ वर्षों में फैला हुआ है ।
उन्होंने बात को जारी रखते हुए कहा: और आप कितना संदेह करेंगे? मैं केवल दो वैज्ञानिकों को जानता हूं जो कहते हैं कि छठा व्यापक विलोपन कुछ नहीं है। अगर हम अगले दो या तीन दशकों के भीतर इस व्यापक विलोपन की घटना पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो हमारा विनाश निश्चित और पूर्ण होगा । वास्तव में, इस बात में क्या तुक है कि आप व्यापक विलोपन के और गंभीर होने की प्रतीक्षा करें ताकि आपको यकीन हो जाए कि व्यापक विलोपन सचमुच हो रहा है? उस समय तक कुछ भी करने का समय बीत चुका होगा। विलोपन की प्रतीक्षा करना और फिर कहना कि अरे, यह तो वास्तव में हो गया बेकार है, क्योंकि तब तक हम जा चुके होंगे । हमको कोई कदम उठाना चाहि ए । अभी ।
विशेष लेख
वनाधिकार अधिनियम और आदिवासी
अनुराग मोदी
लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जंगल को लेकर आए दो फैसलों ने आदिवासियों को बेचैन कर दिया है।
भाजपा की केन्द्र सरकार के प्रति नाराजी पैदा करने वाले इन फैसलों में पहला है, 'वनाधिकार अधिनियम-२००६` पर हाल में आया सुप्रीम कोर्ट का वह आदेश जिसमें करीब १२ लाख आदिवासी परिवारों को उनकी पीढ़ियों की बसाहट से बेदखल किया जाना था । इन आदिवासियों और अन्य पारंपरिक वन-निवासियों के 'वनाधिकार कानून` के तहत किए गए दावे खारिज कर दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश सुनवाई में केन्द्र सरकार की लापरवाही के चलते कई-कई बार आदिवासियों का पक्ष नहीं रखे जाने के कारण आया था।
दूसरा फैसला, चुनाव की घोषणा के ठीक पहले, ७ अप्रेल-मई को 'वन कानून- १९२७` में अंग्रेजों को भी शर्मसार करने वाले संशोधन का प्रस्ताव । हालांकि, दोनों ही मामलों में फिलहाल को कार्यवाही नहीं की जाएगी । पहले मामले में केंद्र सरकार की अंतरिम याचिका के चलते सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई माह तक बेदखली के अपने ही आदेश पर रोक लगा दी है और दूसरे में 'वन कानून-१९२७` में परिवर्तन भी आम चुनाव के बाद ही संभव होगा ।
केन्द्र सरकार के इन आदिवासी विरोधी कदमों को लेकर आदिवासियों के बीच सक्रिय संगठनों ने कमर कस ली है। उनका स्पष्ट मानना है कि यह आदिवासियों के जंगल पर पारंपरिक अधिकारों पर सीधा हमला है। चुनाव के बाद इन दोनों ही मामलों में कार्यवाही होगी, इसलिए देशभर के आदिवासियों ने लोकसभा चुनाव में इसे मुद्दा बनाने का तय कर लिया है। एक अप्रैल को मध्यप्रदेश के बुरहानपुर शहर में 'जागृत आदिवासी दलित संगठन` के बैनर तले आयोजित 'चेतावनी रैली` में एकत्रित हुए पांच हजार आदिवासियों एवं अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों के तेवर से यह बात साफ थी। शहरभर में निकाली गई रैली के बाद हुई आमसभा में इन संगठनों ने कांग्रेस और भाजपा से वन अधिकार के मुद्दे पर अपना पक्ष साफ करने को कहा है। 'वोट हमारा-राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा` का नारा देते हुए इस विशाल जमावडे ने खुलासा कर दिया कि अब आदिवासी चुपचाप आँख मूंदकर अपना वोट नहीं देगा ।
बुरहानपुर में आदिवासियों का सबसे बड़ा सवाल था कि 'वनाधिकार अधिनियम` पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में केन्द्र सरकार मौन क्यों रही ? जबकि सच्च् यह है कि 'वनाधिकार कानून-२००६` के क्रियान्वयन के नाम पर उसकी धज्जियाँ उड़ा जा रही हैं। इस कानून में ग्राम सभाओं को वन अधिकार के दावों की जांच कर पात्रता तय करने का हक है, पर ग्राम सभाओं के बैठने के पहले ही या ग्राम सभाओं के प्रस्तावों को नजरंदाज कर वन विभाग का अमला एवं जिला प्रशासन दावों को अपात्र बता देता है। सामुदायिक वन अधिकार कहीं नहीं दिए गए हैं।
सभा में आदिवासियों ने विस्तार में बताया कि किस तरह पीढ़ियों से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको अपने घर और खेत से उजाड़ा गया है, उनके घर जलाये गए हैं, महिलाओं और बच्चें के साथ भी मार-पीट की गई है, उन्हें जेल में बंद किया गया है, उनके खेत नष्ट किये गए हैं, मवेशी जब्त किये गए हैं । वनाधिकार कानून के तहत यह सब प्रतिबंधित है, पर आज भी ये सिलसिला जारी है और इस गैर-कानूनी आतंक के खिलाफ सभी नेता और प्रशासन मौन हैं।
केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के बेदखली केआदेश के बाद दायर अंतरिम याचिका में खुद ही यह माना है कि दावे को तय करने की प्रक्रिया सही ढंग से नहीं हुई है एवं जिनके दावे खारिज हुए हैं उन्हें सुना भी नहीं गया है। अगर सरकार पहले ही यह पूरी बात कोर्ट के सामने रखती तो बेदखली का आदेश नहीं आता।
मध्यप्रदेश-महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित बुरहानपुर में आयोजित आदिवासियों की आमसभा में कांग्रेस के रवैये पर भी नाराजी जाहिर की गई । उनका सवाल था कि यूपीए सरकार क्यों अपने कार्यकाल में, अपने ही द्वारा लाए गए 'वनाधिकार कानून-२००६` का सही-सही पालन नहीं करवा पाई ? मोदी सरकार के दोनों फैसलों को इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस क्यों प्रमुख चुनावी मुद्दा नहीं बना रही है? जबकि आज मध्यप्रदेश, छतीसगढ़ एवं राजस्थान में कांग्रेसी सरकार आदिवासियों, दलितों की दम पर है । मध्यप्रदेश में ही कांग्रेस के ४१प्रतिशत विधायक आरक्षित वर्ग से हैं ।
'वन कानून-१९२७` ब्रिटिश सरकार के व्यापारिक हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। इस कानून ने आदिवासियों की रोजमर्रा की जरूरतों को अपराधिक करार देते हुए उन्हें अपने ही घर में चोर बना दिया था । इस कानून के आधार पर ही वन विभाग आदिवासी क्षेत्र के लगभग आधे भू-भाग का मालिक बन गया था। वन विभाग को दुनिया का सबसे बड़ा जमींदार और आदिवासियों को गुलाम बनाने वाले इस कानून से मुक्ति पाकर असली आजादी प्राप्त करने के लिए इसमें बड़े बदलाव की जरुरत लम्बे समय से महसूस की जा रही थी। अब, आजादी के ७२ साल बाद इसमें जो बदलाव प्रस्तावित किए जा रहे हैं वे इस कानून को और अत्याचारी बना देंगे।
मसलन-'वन कानून-१९२७` में बदलाव के प्रस्ताव के अनुसार जंगल में अतिक्रमण कर खेती करने,झोपडी बनाने या बिना इजाजत वनोपज लेने, पत्ते बीनने पर होने वाली सजा को एक माह से बढ़ाकर ६ माह किया जाएगा । उसके साथ ही जुर्माने की राशि को ५०० से बढ़ाकर पांच हजार रुपए किया जाएगा। दूसरी बार पकड़ाने पर यह सजा बढ़कर एक साल और जुर्माने की राशि २० हजार से लेकर दो लाख रुपए तक हो जाएगी । इतना ही नहीं, वन विभाग व्दारा बनाए कच्च्े या पक्के पिलर, टीला, फेंसिंग, गड्ढे, रेलिंग आदि किसी भी चीज को नुकसान पहुंचता है, या जगह से हटाया जाता है, तो तीन से सात साल तक की सजा और ५० हजार से ५० लाख रुपए तक का जुर्माना होगा।
'वनाधिकार कानून-२००६` में निस्तार के क्या अधिकार हैं और वो किन-किन लोगों के नाम पर हैं, यह वन विभाग के पास लिखा रहेगा । इसके अलावा अगर जंगल से गिरे हुए पत्ते भी उठाकर लाएंगे तो वन-अपराध में प्रकरण बनेगा। इस तरह के प्रावधान किसी भी कानून में शामिल करना तो दूर, इसके बारे में सोचना भी जन-विरोधी है। किसी भी लोकतांत्रिक देश की सरकार ऐसा कैसे सोच सकती है कि कुपोषण और भुखमरी से पीड़ित को समुदाय हजारों और लाखों रुपयों का जुर्माना भर पाएगा ! इन अपराधों में लोगों को पकड़कर बंद करने के लिए जंगल में वन थाने बनाने का प्रस्ताव भी है।
इतना ही नहीं, हर जिला अदालत में इन मामलों की सुनवाई के लिए अलग से कोर्ट बनाने की भी खा़स व्यवस्था करने की बात है। ऐसे में सहज सवाल उठता है कि ऐसी कौन-सी जरुरत आन पड़ी कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के ठीक दो दिन पहले सरकार ने 'वन कानून-१९२७` में अंग्रेजों को भी शर्मसार करने वाले संशोधन प्रस्तावित किए ?
जाहिर है, केन्द्र की भाजपा सरकार समूचा जंगल कंपनियों को देने की हड़बड़ी में है। हाल ही में छतीसगढ़ में चार लाख एकड जंगल अडानी से जुड़ी एक कंपनी को कोयला निकालने के लिए दिया जा चुका है। बाकी जंगल पर्यावरण बचाने के नाम पर उद्योगों, पूंजीपतियों को दिया जाएगा। सरकार आदिवासियों और वननिवासियों की रोजमर्रा की जरूरतों को भी अपराध मानकर उन्हें जेल में डालने और भारी जुर्माने ठोंकने की तैयारी कर रही है। इस सबके खिलाफ चुनाव के बाद भी आदिवासी और सरकार के बीच कड़े संघर्ष की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता ।
जल जगत
देश, जल संकट से जूझ रहा है
डॉ. आर.बी. चौधरी
भारत के जल संसाधनों के संकट की शुरुआत आंकड़ों से होती है। भारत में जल विज्ञान सम्बंधी आंकड़े संग्रह करने का काम मुख्यत: केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) करता है।
सीडब्ल्यूसी का नाम लिए बगैर नीति आयोग की रिपोर्ट भारत में जल आंकड़ा प्रणाली को कठघरे में खड़ी करती है। नीति आयोग की रिपोर्ट में बातें तो खरी हैं: यह गहरी चिंता की बात है कि भारत में ६० करोड़ से अधिक लोग ज्यादा से लेकर चरम स्तर तक का जल दबाव झेल रहे हैं। भारत में तकरीबन ७० फीसदी जल प्रदूषित है, जिसकी वजह से पानी की गुणवत्ता के सूचकांक में भारत १२२ देशों में १२०वें स्थान पर है ।
हमारे यहां पानी के इस्तेमाल और संरक्षण से जुड़ी कई समस्याएं हैं । पानी के प्रति हमारा रवैया ही ठीक नहीं है। हम इस भ्रम में रहते हैं कि चाहे जितने भी पानी का उपयोग/ दुरुपयोग कर लें, बारिश से हमारी नदियों और जलाशयों में फिर से नया पानी आ ही जाएगा । यह रवैया सरकारी एजेंसियों का भी है और आम लोगों का भी। अगर किसी साल बारिश नहीं होती तो इसके लिए हम जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को जिम्मदार ठहराने लगते हैं ।
पानी के इस्तेमाल के मामले में घरेलू उपयोग की बड़ी भूमिका नहीं है लेकिन कृषि की है। १९६० के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत के बाद से कृषि में पानी की मांग बढ़ी है। इससे भूजल का दोहन हुआ है, जल स्तर नीचे गया है। इस समस्या के समाधान के लिए पर्याप्त् उपाय नहीं किए जा रहे हैं। जब भी बारिश नहीं होती तब संकट पैदा होता है। नदियों के पानी का मार्ग बदलने से भी समाधान नहीं हो रहा है। स्थिति काफी खराब है। इस वर्ष अच्छी वर्षा होने का अनुमान है तो जल संचय के लिए अभी से ही कदम उठाने होंगे। लोगों को चाहिए कि पानी की बूंद-बूंद को बचाएं ।
गर्मियां आते ही जल संकट पर बातें शुरू हो जाती हैं लेकिन एक पूर्व चेतावनी उपग्रह प्रणाली के अध्ययन पर आधारित रिपोर्ट काफी डराने वाली है क्योंकि यह रिपोर्ट भारत में एक बड़े जल संकट की ओर इशारा कर रही है। भारत, मोरक्को, इराक और स्पेन में सिकुड़ते जलाशयों की वजह से इन चार देशों में नलों से पानी गायब हो सकता है। दुनिया के ५ लाख बांधों के लिए पूर्व चेतावनी उपग्रह प्रणाली बनाने वाले डेवलपर्स के अनुसार भारत, मोरक्को, इराक और स्पेन में जल संकट डे जीरो तक पहुंच जाएगा । यानी नलों से पानी एकदम गायब हो सकता है। अध्ययन में कहा गया है कि भारत में नर्मदा नदी से जुड़े दो जलाशयों में जल आवंटन को लेकर प्रत्यक्ष तौर पर तनाव है।
पिछले साल कम बारिश होने की वजह से मध्य प्रदेश के इंदिरा सागर बांध में पानी सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। जब इस कमी को पूरा करने के लिए निचले क्षेत्र में स्थित सरदार सरोवर जलाशय को कम पानी दिया गया तो काफी होहल्ला मच गया था क्योंकि सरदार सरोवर जलाशय में ३ करोड़ लोगों के लिए पेयजल है। पिछले महीने गुजरात सरकार ने सिंचाई रोकते हुए किसानों से फसल नहीं लगाने की अपील की थी।
नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में विश्व की १७ प्रतिशत जनसंख्या रहती है, जबकि इसके पास विश्व के शुद्ध जल संसाधन का मात्र ४ प्रतिशत ही है। किसी भी देश में अगर प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता १७०० घन मीटर से नीचे जाने लगे तो उसे जल संकट की चेतावनी और अगर १००० घन मीटर से नीचे चला जाए, तो उसे जल संकटग्रस्त माना जाता है। भारत में यह फिलहाल १५४४ घन मीटर प्रति व्यक्ति हो गया है, जिसे जल की कमी की चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। नीति आयोग ने यह भी बताया है कि उपलब्ध जल का ८४ प्रतिशत खेती में, १२ प्रतिशत उद्योगों में और ४ प्रतिशत घरेलू कामों में उपयोग होता है।
हम चीन और अमेरिका की तुलना में एक इकाई फसल पर दो से चार गुना अधिक जल उपयोग करते हैं। देश की लगभग ५५ प्रतिशत कृषि भूमि पर सिंचाई के साधन नहीं हैं। ग्यारहवीं योजना के अंत तक भी लगभग १३ करोड़ हैक्टर भूमि को सिंचाई के अंतर्गत लाने का प्रवधान था। इसे बढ़ाकर अधिक-से-अधिक १.४ करोड़ हैक्टर तक किया जा सकता है। इसके अलावा भी काफी भूमि ऐसी बचेगी, जहां सिंचाई असंभव होगी और वह केवल मानसून पर निर्भर रहेगी। भूजल का लगभग ६० प्रतिशत सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाता है। ८० प्रतिशत घरेलू जल आपूर्ति भूजल से ही होती है। इससे भूजल का स्तर लगातार घटता जा रहा है।
लगातार दो वर्षों से मानसून की खराब स्थिति ने देश के जल संकट को गहरा दिया है। आबादी लगातार बढ़ रही है, जबकि जल संसाधन सीमित हैं। अगर अभी भी हमने जल संरक्षण और उसके समान वितरण के लिए उपाय नहीं किए तो देश के तमाम सूखा प्रभावित राज्यों की हालत और गंभीर हो जाएगी। नीति आयोग द्वारा समय-समय पर जल समस्या पर अध्ययन किए जाते हैं किन्तु आंकड़े जिस सच्चई का चित्रण करते हैं उस पर ध्यान देने की तत्काल आवश्यकता है।
जल संरक्षण एवं प्रबंधन के समय-समय पर कई सुझाव दिए जाते हैं किन्तु विशेषज्ञों की राय में निम्नलिखित बातों का स्मरण रखा जाना अति आवश्यकहै। जैसे, लोगों में जल के महत्व के प्रति जागरूकता पैदा करना, पानी की कम खपत वाली फसलें उगाना, जल संसाधनों का बेहतर नियंत्रण एवं प्रबंधन एवं जल सम्बंधी राष्ट्रीय कानून बनाया जाना इत्यादि। हांलाकि, संवैधानिक तौर पर जल का मामला राज्योंसे संबंधित है लेकिन अभी तक किसी राज्य ने अलग-अलग क्षेत्रों को जल आपूर्ति सम्बंधी कोई निश्चित कानून नहीं बनाए हैं।
अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस की घोषणा ब्राजील के रियो दे जनेरो में १९९२ में हुए पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीईडी) में हुई थी। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने २२ अप्रेल-मई को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में घोषित किया । २००५-२०१६ के दशक को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय जल अभियान का दशक घोषित किया था। इसी दशक के तहत पिछले दिनों दक्षिण अफ्रीकी शहर केप टाउन में पानी सूख जाने की खबर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में रही।
पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी का २.६ फीसदी ही साफ पानी है। और इसका एक फीसदी पानी ही मनुष्रू इस्तेमाल कर पाते हैं। वैश्विक पैमाने पर इसी पानी का ७० फीसदी कृषि में, २५ फीसदी उद्योगों में और पांच फीसदी घरेलू इस्तेमाल में निकल जाता है। भारत में साढ़े सात करोड़ से ज्यादा लोग पीने के साफ पानी के लिए तरस रहे हैं। नदियां प्रदूषित हैं और जल संग्रहण का ढांचा चरमराया हुआ है। ग्रामीण इलाकों मे इस्तेमाल योग्य पानी का संकट हो चुका है ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जल उपयोग का प्रति व्यक्ति आदर्श मानक १००-२०० लीटर निर्धारित किया है। विभिन्न देशों में ये मानक बदलते रहते हैं । लेकिन भारत की बात करें तो स्थिति बदहाल ही कही जाएगी, जहां औसतन प्रति व्यक्ति जल उपयोग करीब ९० लीटर प्रतिदिन है। अगर जल उपलब्धता की बात करें, तो सरकारी अनुमान कहता है कि २०२५ तक प्रति व्यक्ति १३४१ घन मीटर उपलब्ध होगा। २०५० में यह और कम होकर ११४० रह जाएगा ।
स्वास्थ्य
देश की स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां
मनीष/स्मृति मिश्रा
आज विज्ञान इस स्तर तक पहुंच चुका है कि मलेरिया और टाइफाइड जैसी संक्रामक बीमारियों का इलाज मानक दवाइयों के नियमानुसार सेवन से किया जा सकता है।
हालांकि भारत में अतिसंवेदनशील आबादी तक अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में अभी भी मलेरिया के कारण मौतें हो रही हैं। एक अप्रभावी उपचार क्रम एंटीबायोटिक-रोधी किस्मों को जन्म दे सकता है। यह आगे चलकर देश की जटिल स्वास्थ्य सम्बंधी चुनौतियों को और बढ़ा देगा ।
भारत में रोग निरीक्षण सहित वर्तमान स्वास्थ्य सेवा प्रणाली अभी भी मध्य युग में हैं। भारत ने आर्थिक रूप से और अंतरिक्ष अन्वेषण जैसे कुछ अनुसंधान क्षेत्रोंमें बेहद उन्नत की है। किन्तु विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की मलेरिया रिपोर्ट २०१७ के अनुसार, भारतीय मलेरिया रोग निरीक्षण प्रणाली केवल ८ प्रतिशत मामलों का पता लगा पाती है, जबकि नाइजीरिया की प्रणाली १६ प्रतिशत मामलों का पता लगा लेती है। इसलिए भारत सरकार बीमारी के वास्तविक बोझ का अनुमान लगाने और उसके आधार पर संसाधन आवंटन करने में असमर्थ है। जबकि किसी भी अन्य राष्ट्र की तरह, भारत को भी सतत विकास के लिए एक स्वस्थ आबादी की आवश्यकता है।
भारत टीकों का सबसे बड़ा निर्माता है। भारत सरकार का राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, हाल ही में शुरू किए गए इंद्रधनुष कार्यक्रम सहित, एक मजबूत प्रणाली है जिसने स्वच्छता एवं स्वास्थ्य सेवा के कमतर स्तर, उच्च तापमान, बड़ी विविध-तापूर्ण आबादी और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद सफलता-पूर्वक पोलियो उन्मूलन का लक्ष्य हासिल किया है। इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा टीकाकरण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए विभिन्न शोध कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं, जैसे इम्यूनाइजेशन डैटा: इनोवेटिंग फॉरएक्शन (आईडीआईए)।
भारत में मूलभूत अनुसंधान उस स्थिति में पहुंच चुका है, जहां वह विकास की चुनौती के बावजूद सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार समाधान विकसित कर सकता है। अकादमिक शोध में कम से कम तीन संभावित मलेरिया वैक्सीन तैयार हुए हैं, जबकि एक भारतीय कम्पनी (भारत बायोटेक) द्वारा हाल ही में डब्ल्यूएचओ प्रीक्वालिफाइड टाइफाइड वैक्सीन विकसित किया गया है। अलबत्ता, आश्चर्य की बात तो यह है कि इस डब्ल्यूएचओ प्रीक्वालिफाइड टाइफाइड वैक्सीन की रोकथाम-क्षमता का डैटा ऑक्यफोर्डविश्ववद्यालय में नियंत्रित मानव संक्रमण मॉडल (उकखच) का उपयोग करके हासिल किया गया है। इसका कारण यह हो सकता है कि भारत में नैदानिक परीक्षण व्यवस्था कमजोर और जटिल है।
भारत की पारंपरिक नैदानिक परीक्षण व्यवस्था बहुत जटिल है। २००५ के बाद से चिकित्सा शोध पत्रिका संपादकों की अंतर्राष्ट्रीय समिति मांग करती है कि किसी भी क्लीनिकल परीक्षण का पूर्व-पंजीकरण (यानी प्रथम व्यक्ति को परीक्षण में शामिल करने से पहले पंजीकरण) किया जाए ताकि प्रकाशन में पक्षपात को रोका जा सके। हालांकि भारत की क्लीनिकल परीक्षण रजिस्ट्री अभी भी परीक्षण के बाद किए गए पंजीकरण को स्वीकार करती है।
ह्यमून पैपिलोमा वायरस (एचपीवी) वैक्सीन के क्लीनिकल परीक्षण पर काफी हल्ला-गुल्ला हुआ था जिसके चलते संसदीय स्थायी समिति और एक विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच हुई, मीडिया में काफी चर्चा हुई और सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि सार्वजनिक विश्वास में गिरावट आई। भारत में एचपीवी परीक्षणों की जांच करने वाली विशेषज्ञ समिति ने पाया कि गंभीर घटनाओं का पता लगाने में हमारी क्लीनिकल अनुसंधान प्रणाली विफल है।
टीकों के उपयोग से रोग का प्रकोप कम हो जाता है जिसके चलते दवा का उपयोग कम करना पड़ता है। इस प्रकार टीकाकरण एंटीबायोटिक प्रतिरोध की समस्या को भी कम कर सकता है। भारत में बेहतर टीकाकरण कार्यक्रम, वैक्सीन उत्पादन सुविधाआेंऔर बुनियादी वैक्सीन अनुसंधान को देखते हुए, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत में वैक्सीन विकास को किस तरह तेज किया जा सकता है? जब हमारे पास टीके की रोकथाम-क्षमता पर पर्याप्त् डैटा न हो तो क्या हम एक बड़ी आबादी को एक संभावित टीका देने का खतरा मोल ले सकते हैं? या क्या यह बेहतर होगा कि पहले अत्यधिक नियंत्रित परिस्थिति में टीकेकी रोकथाम-क्षमता का मूल्यांकन किया जाए और फिर बड़ी जनसंख्या पर परीक्षण शुरू किए जाएं ?
सीएचआईएम (मलेरिया के लिए, नियंत्रित मानव मलेरिया संक्रमण, सीएचएमआई) एक संभावित वैक्सीन की रोकथाम-क्षमता का ठीक-ठाक मूल्यांकन करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, जिसमें बड़े परीक्षण की जरूरत नहीं है। सीएचएमआई में नियंत्रित शब्द अत्यधिक नियंत्रित परिस्थिति का द्योतक है। जैसे भलीभांति परिभाषित परजीवी स्ट्रेन, संक्रमण उन्मूलन के लिए प्रभावी दवा और कड़ी निगरानी के लिए अत्यधिक कुशल निदान प्रणाली। संक्रमण शब्द से आशय है कि परीक्षण के दौरान संक्रमण शुरू किया जाएगा, बीमारी नहीं । शब्द मानव का मतलब है कि प्रयोग इंसानों पर होंगे जैसा कि किसी भी क्लीनिकल टीका अनुसंधान में रोकथाम-क्षमता के आकलन में किया जाता है।
अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, तंजानिया और केन्या जैसे कई देशों में सीएचआईएम अध्ययन करने की क्षमता विकसित की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पिछले २५ वर्षों से सीएचएमआई परीक्षण में १००० से अधिक वालंटियर्स ने भाग लिया है और कोई प्रतिकूल घटना सामने नहीं आई है। पहले संक्रामक बीमारी के लिए हम ज्यादातर दवाइयां/टीके बाहर से मंगाते थे, लेकिन स्थिति तेजी से बदल रही है। उदाहरण के लिए भारत में रोटावायरस टीके का विकास हुआ है।
यह सही है कि स्वदेशी समाधान विकसित करने की बजाय आयात करना हमेशा आसान होता है लेकिन यदि पोलियो टीका भारत में विकसित किया गया होता, तो हम एक पीढ़ी पहले पोलियो से मुक्त हो सकते थे। भारत में सीएचआईएम अध्ययन विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होगी । वर्तमान स्थिति में, यह मलेरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियों के लिए किया जा सकता है लेकिन शायद जीका, डेंगू और टीबी के लिए नहीं। अलबत्ता, यदि उच्चतम मानकों को पालन नहीं किया जा सकता है तो बेहतर होगा कि सीएचआईएम अध्ययन न किए जाएं ।
सीएचआईएम में सबसे बड़ी बाधा लोगों की धारणा की है। इस धारणा को केवल तभी संबोधित किया जा सकता है जब हम सीएचआईएम अध्ययन के लिए वैज्ञानिक, नैतिक और नियामक ढांचा विकसित कर सकें जिसमें बुनियादी अनुसंधान, क्लीनिकल अनुसंधान, नैतिकता, विनियमन, कानून और सामाजिक विज्ञान में सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञता का समावेश हो। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि यह ढांचा सीएचआईएम केलिए उच्चतम मानकों को परिभाषित करे। मीडिया को उनकी मूल्यवान आलोचना और कार्यवाही के व्यापक पारदर्शी प्रसार की अनुमति दी जानी चाहिए।
इसकी शुरुआत किसी सरकारी संगठन द्वारा की जानी चाहिए ताकि जनता में यह संदेह पनपने से रोका जा सके कि यह दवा कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक लाभ के लिए किया जा रहा है। एक या दो उत्कृष्ट अकादमिक संस्थानों को चुना जाना चाहिए और सीएचआईएम अध्ययन करने की क्षमता विकसित की जानी चाहिए । चूंकि संक्रामक बीमारियां निरंतर परिवर्तनशील हैं, भारत में सीएचआईएम अध्ययन पर चर्चा के लिए गहन प्रयासों की तत्काल आवश्यकता है।
पर्यावरण परिक्रमा
प्रेस की आजादी के मामले में भारत की बदतर हालत
रिपोट्र्स विदआउट बार्डर्स की सालाना रिपोर्ट में भारत प्रेस की आजादी के मामले मेंदो पायदान खिसक गया है । १८० देशों में भारत का स्थान १४०वां है । रिपोर्ट में भारत में चल रहे चुनाव प्रचार के दौर को पत्रकारों के लिए खासतौर पर सबसे खतरनाक वक्त के तौर पर चिन्हित किया है ।
सूचकांक मेंकहा गया है कि भारत में प्रेस स्वतत्रंता की वर्तमान स्थिति में से एक पत्रकारों के खिलाफ हिंसा है जिसमें पुलिस की हिंसा, माओवादियों के हमले, अपराधी समूहों या भ्रष्ट राजनीतिज्ञों का प्रतिशोध शामिल हैं । २०१८ में अपने काम की वजह से भारत में छह पत्रकारों की जान गई है । एक मामले में भी यही संदेह हैं ।
इसमें कहा गया है कि ये हत्याएं बताती हैं कि भारतीय पत्रकार कई खतरों का सामना करते हैं, खासतौर पर, ग्रामीण इलाकों में गैर अंग्रेजी भाषी मीडिया के लिए काम करने वाले पत्रकार । विश्लेषण में आरोप लगया गया हे कि २०१९ के आम चुनाव के दौरान सत्तारूढ़ भाजपा के समर्थकोंद्वारा पत्रकारों पर हमले बढ़े हैं ।
पेरिस स्थित रिपोट्र्स सैंन्स फ्रंटियर्स(आरएसएफ) या रिपोट्र्स विदआउट बार्ड्र्स एक गैर लाभकारी संगठन है जो दुनिया भर के पत्रकारोंपर हमलों का दस्तावेजी-करण करने और मुकाबला करने केलिए काम करता है । २०१९ के सूचकांक मेंरिपोट्र्स विदआउट बार्ड्र्स ने पाया कि पत्रकारों के खिलाफ घृणा हिंसा में बदल गई है जिससे दुनिया भर में डर बढ़ा है । भारत के संदर्भ में, इसने हिन्दुत्व को नाराज करने वाले विषयों पर बोलने या लिखने वाले पत्रकारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर समन्वित घृणित अभियानों पर चिंता जताई है । इसने रेखांकित किया है कि जब महिलाआें को निशाना बनाया जाता है तो अभियान खासतौर पर उग्र हो जाता है ।
२०१८ में मीडिया में मी टू अभियान के शुरू होने से महिला संवाददाताआेंके संबंध मेंउत्पीड़न और यौन हमले के कई मामलोेंपर से पर्दा हटा । इसमें कहा गया है कि जिन क्षेत्रों को प्रशासन संवेदनशील मानता है वहां रिपोर्टिंग करना बहुत मुश्किल है जैसे कश्मीर । कश्मीर में विदेशी पत्रकारों को जाने की इजाजत नहीं है और वहां अक्सर इंटरनेट काट दिया जाता है । दक्षिण एशिया से प्रेस की आजादी के मामले में पाकिस्तान तीन पायदान लुढ़ककर १४२वंे स्थान पर है जबकि बांग्लादेश चार पायदान लुढ़ककर १५०वें स्थान पर है । नार्वे लगातार तीसरे साल पहले पायदान पर है जबकि फिनलैंड दूसरे स्थान पर है ।
पहली बार सौर ऊर्जा से दिल्ली मेट्रो ने भरी रफ्तार
प्रदूषण नियंत्रण में दिल्ली मेट्रो की खास पहचान रही है । इस क्रम में प्रदूषण नियंत्रण व पर्यावरण संरक्षण की दिशा में दिल्ली मेट्रो ने एक और बड़ी छलांग लगाई है । मध्यप्रदेश के रीवा में लगाए गए ७५० मेगावाट की क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र (सोलर पावर प्लांट) से दिल्ली मेट्रो को सौर ऊर्जा मिलने लगी है । इसके पहले दिन दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) को रीवा से २७ मेगावाट सौर ऊर्जा की आपूर्ति हुई । इस कारण पहली बार सौर ऊर्जा से मेट्रो ने रफ्तार भरी । इस दौरान वायलेट लाइन पर सौर ऊर्जा े रफ्तार भर रही मेट्रो में डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक मंगू सिंह व रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड के चेयरमैन उपेंद्र त्रिपाठी सहित कई अधिकारियों ने जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम से केंद्रीय सचिवालय तक सफर किया । इसके साथ ही सौर ऊर्जा से मेट्रो का परिचालन शुभारंभ हो गया ।
डीएमआरसी का कहना है कि आगामी दिनों में रीवा से प्रतिदिन ९९ मेगावाट सौर ऊर्जा मिलने लगेगी । इसका इस्तेमाल मेट्रो के परिचालन के साथ-साथ फेज तीन के स्टेशनों, डिपो इत्यादि में भी होगा । रीवा सोलर पावर प्लांट से डीएमआरसी को हर साल ३४ करोड़ यूनिट (एमयू) बिजली किफायती दर पर मिलेगी । वर्ष २०१८-१९ में मेट्रो के परिचालन में १०९.२ करोड़ यूनिट बिजली खपत हुई । इसतिए डीएमआरसी को बिजली के बिल पर बड़ी रकम खर्च करना पड़ता है ।
अब सौर ऊर्जा से दिन में मेट्रो की ६० फीसदी बिजली की जरूरतें पूरी हो जाएंगी । इसके अलावा डीएमआरसी मेट्रो स्टेशनों, इपने आवासीय परिसरों व डिपो की छतों पर सोलर प्लेट लगाकर २८ मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन भी कर रहा है । सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ही १७ अप्रैल २०१७ को डीएमआरसी ने रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, सेलर पावर डेवलपस्र व एमपीपीएमसीएल (मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड) से समझौता किया था । रीवा से डीएमआरसी को जून २०१८ से ही बिजली की आपूर्ति होनी थी पर तकनीकी कारणों से देरी हुई ।
डीएमआरसी ने तैयार की थी संयंत्र की रूपरेखा : रीवा का सौर ऊर्जा संयंत्र दुनिया के बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों में शुमार है । रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड ने यह संयंत्र लगाया है । यह भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एईसीआई), मध्यप्रदेश सरकार, एमपीपीएमसीएल (मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड) व सोलर पावर डेवलपर्स का संयुक्त उपक्रम है । शुरूआत से ही इस परियोजना की रूपरेखा तैयार करने में डीएम-आरसी की अहम भूमिका रही है । इस परियोजना में डीएमआरसी सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा और पहला खरीदार पार्टनर है ।
तलाबों में पनपा था धरती का जीवन
ब्रह्मांड के बारे में वैज्ञानिक लगातार रिसर्च करते रहते हैं, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा सका है कि आखिर पृथ्वी पर जीवन की शुरूआत कैसेहुई ।
वैज्ञानिकों का दावा है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरूआत जल से हुई और कहा जाता रहा है कि महासागर में सबसे पहले जीवन शुरू हुआ होगा । हांलाकि हाल की एक स्टडी में इससे अलग बात कही गई हैं । इसमें कहा गया है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरूआत के लिए छोटे तालाब ज्यादा अनुकूल थे । रिपोर्ट में बताया गया है कि पानी में १० सेंटी मीटर की गहराई में नाइट्रोजन ऑक्साइड की अच्छी मात्रा होती है जो जीवन की शुरूआत के लिए सही वातावरण का निर्माण करती है । मैसाचुसेट्स इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी (एमआईटी) की रिपोर्ट के मुताबिक समंदर की गहराई में नाइट्रोजन आसानी से नही फिक्स होता है और इसलिए लाइफ कैटलाइजिंग मुश्किल होती है । शोधकर्ता सुकृत रंजन ने कहा, जीवन की शुरूआत के लिए नाइट्रोजन फिक्सिंग जरूरी है और यह सागर की गहराई मेंसंभव नहीं है । पानी में नाइट्रोजन मौजूद होता है और उसके टूटने के लिए धरती के महौल की जरूरत होती है । वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन तीन बॉन्ड से बंधी होती है और इसलिए इसके टूटने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है ।
उन्होेंने कहा कि उस समय वायुमंडल में लाइटिंग के जरिए नाइट्रोजिन फिक्स होकर महासागर मेंबारिश के जरिए गिरकर जीवन की शुरूआत कर सकता था लेकिन यह इसलिए नहींसंभव लगता है क्योंकि महासागर में नीचे मौजूद आयरन इस फिक्स्ड नाइट्रोजन से जीवन के कारक खत्म कर देता । जीवन के लिए सभी जरूरतेंकेवल उथले जल मेंही पूरी हो सकती थी । उनका कहना है कि तालाब में नाइट्रोजन ऑक्साइड का अच्छा कॉन्संट्रेशन बन सकता है । तालाब में अल्ट्रा वॉइलट रेज और आयरन का भी प्रभाव कम होता है इसलिए नाइट्रोजन आरएनए से लिकर जीवन की शुरूआत करने में ज्यादा सक्षम होता है ।
दशकों की खोज के बाद ब्राह्मंड
ब्रह्मांड निर्माण की रासायनिक क्रिया का पहला सबूत मिल गया है । वैज्ञानिकों ने सुदूर अंतरिक्ष में हीलियम हाइड्राइड आयन का अणु खोज निकाला है । माना जाता है कि ब्रह्मांड के विकासक्रम में सबसे पहले यहीं अणु बना था । इसी ने आगे चलकर आणविक हाइड्रोजन के निर्माण का रास्ता खोला और ब्रह्मांड वर्तमान स्वरूप में आया ।
दशकों से वैज्ञानिक अंतरिक्ष में हीलियम हाइड्राइड आयन को खोजने की कोशिश कर रहे हैं । जिस अणु का ब्रह्मांड निर्माण की रासायनिक क्रियाका मूल कहा जाता है, अंतरिक्ष में कहीं भी उसका प्रमाण नहीं मिलने से ब्रह्मांड निर्माण को लेकर स्थापित पूरे सिद्धांत पर सवालिया निशान लगते रहे हैं । अब एक गैसीय बादल (नेबुला) एनजीसी ७०२७ में इस अणु का प्रमाण मिला है ।
फ्लाइंग ऑब्जर्वेटरी सोफिया पर स्थापित फार इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर ग्रेट की मदद से वैज्ञानिकोंने इस अणु को खोजा है । अमेरिका की जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डेविड न्यूफेल्ड ने कहा, हीलियम हाइड्राइड आयन की खोज बेहद अहम है । प्रकृति मेंअणु निर्माण की व्यवस्था का यह खूबसूरत उदाहरण है । वैज्ञानिकों का कहना है कि इस अणु के मिलने से दशकों पुरानी खोज का सुखद अंत हुआ है । इससे ब्रह्मांड निर्माण के रासयनिक सिद्धांत पर लनेग वाले सवालिया निशान भी हट गए हैं । ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है ।
विज्ञान समाचार
हिमनद झील की भविष्यवाणी
डॉ.दीपक कोहली
इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस, बेगलुरू के वैज्ञानिकों ने हिमनद झीलों के फैलने और फूटने की भविष्यवाणी करने की एक नई तकनीक विकसित की है। वास्तव में हिमनद झीलें तब बनती हैं जब हिमनद खिसकने से खोखली जगहों में बर्फ के बड़े जमाव रह जाते हैं जिनके पिघलने से झीलों का निर्माण होता है।
अध्ययन के लिए सिक्किम की सबसे बड़ी झील, दक्षिण ल्होनाक झील, पर इस नई तकनीक को लागू किया गया । वैसे तो यह झील पहले से ही संभावित खतरे की श्रेणी में है और इस तकनीक के उपयोग से इस बात कि पुïि भी हो गई। नेचर इंडिया में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दिवेचा सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज के वैज्ञानिक रेम्या नंबूदिरी ने सिक्किम स्टेट काउंसिल आफ साइंस एंड टेक्नॉbॉजी केसाथ किए गए अध्ययन में बताया कि इस झील का आकार तेजी से बढ़ रहा है जो आने वाले संभावित खतरे की ओर इशारा करता है।
शोधकर्ताओं का अनुमान है कि 51.4 मीटर गहरी झील का आयतन 2015 में लगभग 6 करोड़ क्यूबिक मीटर था जो बढ़कर 9 करोड़ क्यूबिक मीटर होने की संभावना है। यदि यह झील फूट गई तो इतनी बड़ी मात्रा में पानी के अचानक बहाव से निचले इलाके में खतरनाक हालात बन सकते हैं । पूर्व में हिमालयी क्षेत्र में कई बार प्रलय की स्थिति बन चुकी है । जैसे 1926 का जम्मू-कश्मीर जलप्रलय, 1981 में किन्नौर घाटी, हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और 2013 में केदारनाथ, उत्तराखंड का प्रकोप ।
हिमनद में छिपी इन झीलों पर उपग्रहों की मदद से लगातार नजर रखी जा रही है। किन्तु रिमोट सेंसिंग से न तो झीलों की गहराई का पता लगाया जा सकता है और न ही आपदा के संभावित समय का, इसलिए शोधकर्ताओं ने झीलों के आयतन और उसके विस्तार का अनुमान और असुरक्षित स्थानों की पहचान करने के लिए हिमनद की सतह का वेग, ढलान और बर्फ के प्रवाह जैसे मापदंडों का उपयोग करते हुए एक तकनीक विकसित की है।
उन्होंने इस क्षेत्र में नौ अन्य हिमनद झीलों और तीन स्थलों का भी चित्रण किया है जहां भविष्य में नई झीलें बन सकती हैं। रिपोर्ट के अनुसार, इस तकनीक का उपयोग हिमालय के अन्य हिमनदों की निगरानी के लिए भी किया जा सकता है ताकि लोगों को अचानक आने वाली बाढ़ के बारे में पहले से चेतावनी दी जा सके ।
खेती के बाद शामिल हुए नए अक्षर:
बातचीत में हम फ और व अक्षरों का आसानी से उच्चारण कर लेते हैं । लेकिन एक समय था जब इन अक्षरों का उƒारण करना इतना आसान न था, बल्कि ये अक्षर तो भाषा में शामिल भी नहीं थे। हाल ही में नेचर इंडिया में प्रकाशित एक अध्ययन कहता है कि मानवों में फ और व बोलने की क्षमता, खेती के फैलने और मानवों द्वारा पका हुआ भोजन खाने की संस्कृति की बदौलत विकसित हुई है ।
1985 में अमेरिकी भाषा विज्ञानी चाल्र्स हॉकेट ने इस ओर ध्यान दिलाया था कि हजारोंवर्ष पहले शिकारियों की भाषा में दंतोðç ध्वनियां शामिल नहीं थीं। उनका अनुमान था कि इन अक्षरों की कमी के लिए आंशिक रूप से उनका आहार जिम्मेदार था। उनके अनुसार खुरदरा और रेशेदार भोजन चबाने से जबड़ों पर जोर पड़ता है जिसके कारण दाढ़ें घिस जाती हैं। इसके फलस्वरूप निचला जबड़ा बड़ा हो जाता है। इस तरह धीरे-धीरे ऊपरी और निचला जबड़ा और दांत एक सीध में आ जाते हैं। दांतों की इस तरह की जमावट के कारण ऊपरी जबड़ा नीचे वाले होंठ को छू नहीं पाता। दंतोðç ध्वनियों के उƒारण के लिए ऐसा होना जरूरी है।
डैमियल ब्लैसी और स्टीवन मोरान और उनके साथियों ने अपने अध्ययन में चाल्र्स हॉकेट के इस विचार को जांचा । अध्ययन के अनुसार मानव द्वारा मुbायम (पका हुआ) भोजन खाने से जबड़ों पर कम दबाव पड़ा। कम दबाव पड़ने के कारण उनका ऊपरी जबड़ा निचले जबड़े की सीध में न होकर निचले जबड़े को थोड़ा ढंकने लगा । जिसके कारण इन ध्वनियों को बोलने में आसानी होने लगी और भाषा में नए शब्द जुड़े ।
अध्ययनकर्ताओं ने हॉकेट के विचार को जांचने के लिए कम्प्यूटूटर मॉडलिंग की मदद ली । इसकी मदद से उन्होंने यह दिखाया कि ऊपरी और निचले दांतों के ठीक एक के ऊपर एक होने की तुलना में जब ऊपरी और निचले दांत ओवरलैप (ऊपरी जबड़ा निचले जबड़े को ढंक लेता है) होते हैं तो दंतोðç (फ और व) ध्वनि के उच्चारण में 29 प्रतिशत कम जोर लगता है। इसके बाद उन्होंने दुनिया की कई भाषाओं की जांच की । उन्होंने पाया कि कृषि आधारित सभ्यताओं की भाषा की तुbना में शिकारियों के भाषा कोश में सिर्फ एक चौथाई दंतोðç अक्षर थे। इसके बाद उन्होंने भाषाओं के बीच के सम्बंध को देखा और पाया कि दंतोðç ध्वनियां तेजी से फैbती हैं। इसी कारण ये अक्षर अधिकांश भाषाओं में मिल जाते हैं ।
इस अध्ययन के नतीजे इस बात की ओर भी इशारा करते हैं कि जीवन शैली में बदलाव हमें कई तरह से प्रभावित कर सकते हैं, ये हमारी भाषा को भी प्रभावित कर सकते हैं।
ब्लैक होल की सहायता से अंतरिक्ष यात्रा :
किसी कल्पित एलियन सभ्यता द्वारा यात्रा करने के तरीके क्या होंगे ? कोलंबिया विश्वविद्यालय के एक खगोल विज्ञानी ने कुछ अटकल लगाई है। उनके अनुसार एलियन इसके लिए बायनरी ब्लैक होल पर bेजर से गोलीबारी करके ऊर्जा प्राá कर सकते हैं । गौरतलब है कि बायनरी ब्लैक होल एक-दूसरे की परिक्रमा करते हैं। दरअसल, यह नासा द्वारा दशकों से इस्तेमाल की जा रही तकनीक का ही उन्नत रूप है।
फिलहाल अंतरिक्ष यान सौर मंडल में ग्रेविटी वेल का उपयोग गुलेल के रूप में करके यात्रकरते हैं। पहले तो अंतरिक्ष यान ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और अपनी गति बढ़ाने के लिए ग्रह के करीब जाते हैं। जब गति पर्याá बढ़ जाती है तो इस ऊर्जा का उपयोग वे अगले गंतव्य तक पहुंचने के लिए करते हैं ।
यही सिद्धांत ब्लैक होल के आसपास भी लगाया जा सकता है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होता है। लेकिन यदि कोई फोटॉन ब्लैक होल के नजदीक एक विशेष क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो वह ब्bैक होल के चारों ओर एक आंशिक चक्कर पूरा करके उसी दिशा में लौट जाता है। भौतिक विज्ञानी ऐसे क्षेत्रों को ‘गुरुत्व दर्पण’ और ऐसे लौटते फोटॉन को बूमरैंग फोटॉन कहते हैं।
बूमरैंग फोटॉन पहले से ही प्रकाश की गति से चल रहे होते हैं, इसलिए ब्लैक होल के पास पहुंचकर उनकी गति नहीं बढ़ती बल्कि उन्हें ऊर्जा प्राá हो जाती है। फोटॉन जिस ऊर्जा के साथ गुरुत्व दर्पण में प्रवेश लेते हैं, उससे अधिक ऊर्जा उनमें आ जाती है। इससे ब्लैक होल के संवेग में जरूर थोड़ी कमी आती है।
कोलंबिया के खगोलविद डेविड किपिंग ने आर्काइव्स प्रीप्रिंट जर्नल में प्रकाशित एक पेपर में बताया है कि यह संभव है कि कोई अंतरिक्ष यान किसी बायनरी ब्bैक होल सिस्टम पर bेजर से फोटॉन की बौछार करे और जब ये फोटॉन ऊर्जा प्राप्त कर लौटें तो इनको अवशोषित कर अतिरिक्त ऊर्जा को गति में परिवर्तित कर दे। पारंपरिक लाइटसेल की तुbना में यह तकनीक अधिक लाभदायक होगी क्योंकि इसमें ईंधन की आवश्यकता नहीं है।
किपिंग के अनुसार हो सकता है आकाशगंगा में कोई ऐसी सभ्यता हो जो यात्रा के लिए इस तरह की प्रणाली का उपयोग कर रही हो।
पिघलते एवरेस्ट ने जाहिर किए कई राज :
माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचना हमेशा से एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है। इसके शिखर पर पहुंचने का रास्ता जितना रहस्यों से भरा है उतना ही बाधाओं से भी भरा है। गिरती हुई बर्फ, उबड़ खाबड़ रास्ते, कड़ाके की ठंड और अजीबो-गरीब ऊंचाइयां इस सफर को और चुनौतीपूर्ण बनाती हैं। अभी तक जहां लगभग 5,000 लोग सफलतापूर्वक पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुके हैंवहीं ऐसा अनुमान है कि 300 लोग रास्ते में ही मारे गए हैं ।
पिछले वर्ष शोधकर्ताओं के एक समूह ने एवरेस्ट की बर्फ को औसत से अधिक गर्म पाया। इसके अलावा चार साल से चल रहे एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि बर्फ पिघलने से पर्वत पर तालाबों के क्षेत्र में विस्तार भी हो रहा है। यह विस्तार न केवb हिमनदों के पिघलने से हुआ है बल्कि नेपाल में खम्बु हिमनद की गतिविधि के कारण भी हुआ है।
अधिकांश शव पहाड़ के सबसे खतरनाक क्षेत्रों में से एक, खम्बु में जमे हुए जल प्रपात वाले इलाके में पाए गए । वहां बर्फ के बड़े-बड़े खंड अचानक से ढह जाते हैं और हिमनद प्रति दिन कई फीट नीचे खिसक जाते है। । 2014 में, इस क्षेत्र में गिरती हुई बर्फ के नीचे कुचल जाने से 16 पर्वतारोहियों की मौत हो गई थी।
पहाड़ से शवों को निकालना काफी खतरनाक काम होने के साथ कानूनी अड़चनों से भरा हुआ है। नेपाल के कानून के तहत वहां किसी भी तरह का काम करने के लिए सरकारी एजेंसियों को शामिल करना आवश्यक होता है।
मेंढक की नई प्रजाति मिली :
हाल ही में केरb के वायनाड़ जिbे के पश्चिमी घाट इलाके में वैज्ञानिककें को मेंढक की नई प्रजाति मिली है। इन मेंढकों के पेट नारंगी रंग के हैं। और शरीर के दोनों तरफ हल्के नीले सितारों जैसे धब्बे हैं और उंगलियां तिकोनी हैं । शोधकर्ताओं ने नेचर इंडिया पत्रिका में बताया है कि इन मेंढकों को छुपने में महारत हासिल है। जरा-सा भी खटका या सरसराहट होने पर ये उछल कर पत्ते या घास के बीच छुप जाते हैं।
चूंकि इनके शरीर पर सितारानुमा धब्बे हैं और ये कुरूचियाना जनजाति बहुb वायनाड़ जिbे में मिले हैं,इसलिए शोधकर्ताओं ने इन मेंढकों को एस्टोबेटेकस कुरूचियाना नाम दिया है।
मेंढक की यह प्रजाति सबसे पहले 2010 में इंडियन इंस्टीटçूट आफ साइंस के एस.पी. विजयकुमार ने पहचानी थी। बारीकी से अध्ययन करने पर पता चला कि ये पश्चिमी घाट के अन्य मेंढकों की तरह नहीं है। इसके बाद उन्होंने युनिवर्सिटी आफ फलोरिडा के डेविड ब्bैकबर्न और जॉर्ज वाशिंगटन युनिवर्सिटी के एलेक्स पायरॉन की मदद से मेंढक की हड्डियों और जीन का विश्लेषण किया। हड्डियों की जांच में उन्होंने पाया कि यह मेंढ़क निक्टिबेटेकिडी कुb का है । इस कुb के मेंढकों की लगभग 30 प्रजातियां भारत और श्रीbंका में पाई जाती हैं। और जेनेटिक विश्लेषण से लगता है कि ये मेंढक 6-7 करोड़ वर्ष पूर्व अपनी करीबी प्रजातियों से अलग विकसित होने शुरू हुए थे ।
इस नई प्रजाति के सामने आने से पश्चिमी घाट जैव विविधता के हॉटस्पॉट के रूप में सामने आया है । इससे यहां के जैव विविधता के पैटर्न को समझने में मदद मिलेगी ।
जन जीवन
वृक्ष संस्कार से मृत्यु भी सार्थक
कुमार सिद्धार्थ
मृत्यु के बाद पार्थिव शरीर को आग के हवाले करने की परंपरा के चलते भारत में हर साल ७० फीसदी लकड़ी केवल शवों के अंतिम संस्कार के लिए जला दी जाती है ।
इसके लिए पांच करोड़ पेड़ों को काट कर ४ मिलियन टन लकड़ी प्राप्त की जाती है। पारंपरिक तरीकों के दाह संस्कार से लकड़ी के जलने से हवा में लगभग अस्सी लाख टन कार्बन मोनो-ऑक्साइड या ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। दहन के बाद निकलने वाली राख जलाशयों या नदियों में फेंकी जाती है, जिससे उनकी विषाक्तता बढ़ती है।
कुछ समय पहले राष्ट्रीय हरित पंचाट (ग्रीन ट्रिब्यूनल) ने न केवल दाह-संस्कार के तरीकों पर चिंता प्रकट की थी, बल्कि इन तरीकों से पर्यावरण को होने वाले नुकसान की भी चर्चा की थी । ऐसे में जब दुनिया में पर्यावरण असंतुलन पर गंभीर विमर्श हो रहा हो, तब अंतिम संस्कार के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई समस्या बनकर उभर रही है।
उल्लेखनीय है कि एक शव की अंत्येष्ठि में करीब पांच क्विंटल लकड़ी लगती है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक देश में १.२ प्रतिशत मृत्यु दर है। इस लिहाज से देश में हर साल लगभग १ करोड़ शवों का दाह संस्कार किया जाता है। प्रत्येक शव के अंतिम संस्कार के लिए १५ साल के दो पेड़ अग्नि के हवाले करने पड़ते हैं। लकड़ी से शव के अंतिम संस्कार पर करीब पांच हजार रुपए औसतन खर्च होता है।
वैसे तो देश-दुनिया में पर्यावरण संतुलन एवं हरियाली बनाये रखने के लिए समाज के द्वारा मृत्यु-संस्कार के संदर्भ में वैकल्पिक प्रयास किये जाते रहे हैं। दाह-संस्कार के इन परंपरागत विकल्पों के अलावा `वृक्ष जीवन से मृत्यु-संस्कार` का विचार भी एक विकल्प के रूप में सामने आया है। यह प्रगतिशील विचार सर्वोदय जगत में मशहूर, रचनात्मक चिन्तक, लेखक ८४ वर्षीय भाई मणीन्द्रकुमार के मन में उपजा । मणीन्द्र भाई ने पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने और अंतिम-संस्कार को जीवन उपयोगी बनाने के लिये 'वृक्ष जीवन संस्कार` का सार्थक तरीका अपनाया है, जो मृत्यु संस्कारों की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।
एक मई, २०१८ को मणीन्द्र भाई की पत्नी श्रीमती मोहना देवी का देहावसान हो गया था। दो मई को उनका `वृक्ष संस्कार` सेवाधाम आश्रम, उज्जैन में किया गया । वृक्ष संस्कार के इस तरीके में पहले करीब ६ फीट गहरा और ४ फीट चौडा गड्डा खोदा गया । उसमें पहले गोबर, गौ मूत्र और पेड़ों की पत्तियां डाली गइंर् और उसके ऊपर मिट्टी का बिछौना बनाया गया। उसमें श्रीमती मोहना देवी केशव को लिटाया गया और गड्ढे को फिर मिट्टी से भर दिया गया । इसमें मृत शरीर का भूमि संस्कार कर उसके ऊपर पौधे का रोपण किया गया । मणीन्द्र भाई का मानना है कि मृत शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस एवं अनेक प्रकार के खनिज द्रव्य और अस्थि मज्जा (बोनमेरो) होते हैंजो एक खाद्य के रूप में उपयोगी हो सकते हैं । भूमि संस्कार के बाद शरीर खाद में बदल जाता है और ठीक उसके ऊपर उगने वाला पौधा उस खाद से आवश्यक तत्व ग्रहण कर वृक्ष बन जाता है जो सालों तक मृत व्यक्ति की याद के रूप में जीवित रहता है।
उल्लेखनीय है कि मणीन्द्र कुमारजी के पिता का निधन करीब ३० साल पहले हुआ तो अनायास उनके मन में 'वृक्ष जीवन संस्कार` का विचार आया था । उस वक्त उन्होंने अपने चारों भाईयों से चर्चा की कि पिताजी को अंजड़ (बड़वानी) स्थित जिनिंग फैक्टरी की जमीन पर गाड़कर पांच भाईयों के नाम पर पांच वृक्ष लगा दिये जाएं । लंबे विचार-विमर्श के बाद सभी भाई तो मान गए परन्तु महिलाओं की सहमति नहीं मिल सकी। तब मणीन्द्र भाई ने अग्नि संस्कार में शामिल नहीं होने की घोषणा कर दी, लेकिन परिवारजनों ने तब भी उनकी बात नहीं सुनी । पिता का अग्नि संस्कार ही किया गया । अपने विचार पर अडिग मणीन्द्र कुमार पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए । इसके बाद उन्होंने `वृक्ष जीवन संस्कार` को एक अभियान के रूप में अपनाया, जो अब 'वृक्ष जीवन संस्कार परिषद` के रूप मेंसामने है।
प्रसिद्ध समाजसेवी बाबा आमटे ने भी अपने जीवनकाल में महाराष्ट्र के आनन्द वन में इस प्रक्रिया को प्रारम्भ कर दिया था। वे कई लोगों का वृक्ष संस्कार कर चुके थे, जब बाबा आमटे और उनकी पत्नी साधना ताई का देहान्त हुआ तो उनके परिजनों ने भी इसी अनुसार `वृक्ष संस्कार` किया था । उनका मानना था कि इस विधि से अंतिम संस्कार करने से मनुष्य के सारे अवयवों और यहां तक कि बोनमेरो का भी सार्थक उपयोग हो जाता है। तीन जनवरी २०१२ को वरिष्ठ सर्वोदयी श्याम बहादुर 'नम्र` का मरणोपरान्त वृक्ष संस्कार ही किया गया ।
करीब तीन दशक से 'वृक्ष संस्कार` में लगे मणीन्द्र भाई ने बाबा आमटे की प्रेरणा से इसे एक अभियान का स्वरूप दिया है। बाबा का मानना था कि इस विधि से अंतिम संस्कार करने से दुनिया का भला होगा । मृत्यु संस्कार के इस विकल्प पर अब तक ३०० व्यक्तियों ने अपनी रूचि दिखाते हुए मृत्यु इच्छापत्र पर हस्ताक्षर किये हैं। रतलाम के निकट रत्नेश्वर रोड़, खलघाट, बड़वानी तथा सेवाधाम, उज्जैन में `वृक्ष संस्कार से अंतिम संस्कार` करने की शुरूआत हो चुकी है । बड़वानी नगर पालिका परिषद् ने इस संबंध में प्रस्ताव पारित कर वृक्ष संस्कार करने वालों को जमीन उपलब्ध करवाने की स्वीकृति दी है। पिछले दिनों इंदौर के प्रबुद्धजनों ने इस विचार को कार्यान्वित करने के लिए भूमि खरीदने का विचार किया है। एक सोसायटी गठित कर वृक्ष संस्कार के विचार को कार्यान्वित करने के बारे में सोचा जा रहा है।
वृक्ष जीवन संस्कार परिषद के अध्यक्ष मणीन्द्र भाई कहते हैं कि निकट भविष्य में यह विचार समाज स्वीकार करेगा, क्योंकि वृक्ष संस्कार से मृत्यु भी सार्थक हो जाती है। इससे मृत व्यक्ति न केवल अमर हो जाता है, वह अनन्त भी हो जाता है। वृक्ष के जो बीज होते हैं, वे गिरकर, फिर बढें़गे एवं फैलते जाएंगे। वे बीज फिर वृक्ष बनेंगे और वृक्ष बनने की प्रक्रिया चलती और बढ़ती जाएगी ।
विज्ञान जगत
होमो सेपिएंस धर्म और विज्ञान
गंगानंद झा
क्रमिक जैव विकास के फलस्वरूप आज से लगभग पच्चीस लाख साल पहले मानव के विकास की श्रृंखला की शुरुआत अफ्रीका में होमो वंश के उद्भव के साथ हुई । फिर काल क्रम में इसकी कई प्रजातियां विकसित हुइंर् और अंत में आधुनिक मानव प्रजाति (होमो सेपिएंस) का विकास आज से करीब दो लाख वर्ष पूर्व पूर्वी अफ्रीका में हुआ।
आधुनिक मनुष्य के इतिहास की शुरुआत आज से सत्तर हजार पहले संज्ञानात्मकक्र ांति के रूप में हुई जब उसने बोलने की, शब्द गठन करने की क्षमता पाई । और तब वह अपने मूल स्थान से अन्य क्षेत्रों- युरोप, एशिया वगैरह में पसरता गया ।
इतिहास का अगला पड़ाव करीब १२ हजार साल पहले कृषि क्रांति के साथ आया, जब मनुष्य ने खेती करना शुरू किया । मनुष्य अब यायावर नहीं रह गया, वह स्थायी बस्तियों में रहने लगा । सभ्यता और संस्कृति के विकास की कहानियां बनने लगीं।
अब जब मनुष्य ने समझने और अपनी समझ जाहिर करने की क्षमता हासिल कर ली थी, तो उसने अपने चारों ओर के परिवेश के साथ अपने रिश्ते को समझने की कोशिश की । धरती, आसमान और समंदर को समझने की कोशिश की । जानकारियां इकट्ठी होती चली गइंर् । ये जानकारियां विभिन्न समय में अनेक धाराओं में प्रतिष्ठित हुई । ये धाराएं धर्म कहलाइंर् । अब मनुष्य के पास अपनी समस्याओं, कौतूहल और सवालों के जवाब पाने का एक जरिया हासिल हो गया था।
जीवनयापन के लिए आवश्यक सारी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राचीन काल के मनीषियों द्वारा हमें धार्मिक ग्रंथों अथवा मौखिक परंपराओं में उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। मान्यता यह बनी कि इन ग्रंथों और परंपराओं के समीचीन अध्ययन और समझ के ज़रिए ही हम ज्ञान प्राप्त् कर सकते हैं। लोगों की आस्था थी कि वेद, कुरान और बाइबिल जैसे धर्मग्रंथों में विश्व ब्रह्मांड के सारे रहस्यों का विवरण उपलब्ध है। इन धर्मग्रंथों के अध्ययन या किसी जानकार, ज्ञानी व्यक्ति से संपर्क करने पर सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे । इसलिए नया कुछ आविष्कार करने की जरूरत नहीं रह गई है।
जिम्मेदारी के साथ कहा जा सकता है कि सोलहवीं सदी के पहले मनुष्य प्रगति और विकास की आधुनिक अवधारणा में विश्वास नहीं करते थे। उनकी समझ थी कि स्वर्णिम काल अतीत में था और विश्वअचर है। जो पहले नहीं हुआ, वह भविष्य में नहीं हो सकता । युगों की प्रज्ञा के श्रृद्धापूर्वक अनुपालन से स्वर्णिम अतीत को वापस लाया जा सकता है और मानवीय विदग्धता हमारी रोजमर्रा जिन्दगी के कई पहलुओं में सुधार जरूर ला सकती है लेकिन दुनिया की बुनियादी समस्याओं से उबरना मनुष्य की कूवत में नहीं है। जब सर्वज्ञाता बुद्ध, कन्फ्यूशियस, ईसा मसीह, और मोहम्मद तक अकाल, भुखमरी, रोग और युद्ध रोकने में नाकामयाब रहे तो इन्हें रोकने की उम्मीद करना दिवास्वप्न ही है।
हालांकि तब की सरकारें और सम्पन्न महाजन शिक्षा और वृत्ति के लिए अनुदान देते थे, किन्तु उनका उद्देश्य उपल्बध क्षमताओं को संजोना और संवारना था, न कि नई क्षमता हासिल करना । तब के शासक पुजारियों, दार्शनिकों और कवियों को इस आशा से दान दिया करते थे कि वे उनके शासन को वैधता प्रदान करेंगे और सामाजिक व्यवस्था को कायम रखेंगे। उन्हें इनसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं रहती थी कि वे नई चिकित्सा पद्धति का विकास करेंगे या नए उपकरणों का आविष्कार करेंगे और आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करेंगे । सोलहवीं शताब्दी से जानकारियों की एक स्वतंत्र धारा उभरी । इसे वैज्ञानिक धारा के रूप में पहचाना जाता है।
वैज्ञानिक क्रांति ने सन १५४३ में कॉपर्निकस की विख्यात पांडुलिपि डी रिवॉल्युशनिबस ऑर्बियम सेलेस्चियम (आकाशीय पिंडों की परिक्रमा) के प्रकाशन के साथ आहट दी थी। इस पांडुलिपि ने स्पष्टता के साथ ज्ञान की पारंपरिक धाराओं की स्थापित मान्यता (कि पृथ्वी ब्राह्मांड का केन्द्र है) के साथ अपनी असहमति की घोषणा की। कॉपर्निकस ने कहा कि पृथ्वी नहीं, बल्कि सूर्य ब्राह्मांड का केन्द्र है। पारंपरिक प्रज्ञा के साथ असहमति वैज्ञानिक नजरिए की पहचान है।
कॉपर्निकस की पांडुलिपि के प्रकाशन के २१ साल पहले मेजेलान का अभियान पृथ्वी की परिक्रमा कर स्पेन लौटा था। इससे यह स्थापित हुआ कि पृथ्वी गोल है । इससे इस विचार को आधार मिला कि हम सब कुछ नहीं जानते । नई जानकारियां हमारी जानकारियों को गलत साबित कर सकती हैं। कोई भी अवधारणा, विचार या सिद्धांत ऐसा नहीं होता जो पवित्र और अंतिम हो और जिसे चुनौती न दी जा सके ।
अगली सदी में फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने देकार्ते ने वैज्ञानिक तरीकों से सारे स्थापित सत्य की वैधता का परीक्षण करने की वकालत की। अंतत: सन १८५९ में चार्ल्स डार्विन द्वारा प्राकृतिक वरण से विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किए जाने के साथ ही वैज्ञानिक विचारधारा को व्यापक स्वीकृति और सम्माननीयता मिली।
विज्ञान का वक्तवय है कि डार्विन ने कभी नहीं दावा किया कि वे जीव वैज्ञानिकों की आखिरी मोहर हैं और उनके पास सारे सवालों के अंतिम जवाब हैं। धर्म का आधार आस्था है, विज्ञान का आधार है परंपरा से मिली प्रज्ञा से असहमति । विज्ञान सवाल पूछने को प्रोत्साहित करता है, जबकि धर्म सवाल उठाने को निरुत्साहित करता है।
आधुनिक विज्ञान का आधार यह स्वीकृति है कि हम सब कुछ नहीं जानते । और भी अधिक महत्वपूर्ण है कि विज्ञान स्वीकार करता है कि नई जानकारियां हमारी जानकारियों को गलत साबित कर सकती हैं । विज्ञान अज्ञान को कबूल करने के साथ-साथ नई जानकारियां इकट्ठा करने का लक्ष्य रखता है।
ज्ञान विज्ञान
बर्फ के नीचे छिपे महासागर की खोज
जुलाई २०१७ में, अंटार्कटिक प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में लार्सन सी आइस शेल्फ से एक विशाल हिमखंड टूट गया था । इसके टूटने के साथ ही वर्षों से बर्फ के नीचे ओझल समुद्र की एक बड़ी पट्टी सामने आ गई । इस समुद्र में जैव विकास और समुद्री जीवों की गतिशीलता तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति उनकी प्रतिक्रिया के सुराग मिल सकते हैं।
जर्मनी के अल्फ्रेड वेगेनर इंस्टीट्यूट फॉर पोलर एंड मरीन रिसर्च के वैज्ञानिक बोरिस डोर्सेल के नेतृत्व में ४५ वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम इस समुद्र की खोजबीन के लिए रवाना होने की योजना बना रही है । किन्तु इस दूरस्थ क्षेत्र तक पहुंचना और इतने कठिन मौसम में शोध करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, अलबत्ता यह काफी रोमांचकारी भी होगा ।
लार्सन सी से अलग हुआ बर्फ का यह टुकड़ा ५,८०० वर्ग किलोमीटर का है और २०० किलोमीटर उत्तर की ओर बह चुका है । वैज्ञानिक यह जानने को उत्सुक है कि कौन सी प्रजातियां बर्फ के नीचे पनप सकती हैं, और उन्होंने अचानक आए इस बदलाव का सामना कैसे किया होगा । छानबीन के लिए पिछले वर्ष कैंब्रिज विश्वविद्यालय की जीव विज्ञानी कैटरीन लिनसे की टीम का वहां पहुंचने का प्रयास समुद्र में जमी बर्फ के कारण सफल नहीं हो पाया था। परिस्थिति अनुकूल होने पर नई टीम वहां समुद्र और समुद्र तल के नमूने तो ले पाई, लेकिन ज्यादा आगे नहीं जा पाई ।
अल्फ्रेड वेगेनर इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित पोलरस्टर्न जर्मनी का प्रमुख धु्रवीय खोजी पोत है और दुनिया में सबसे अच्छा सुसज्जित अनुसंधान आइसब्रोकर है। इसमें मौजूद दो हेलीकॉप्टर सैटेलाइट इमेजरी और उड़ानों का उपयोग करके बर्फ की चादर में जहाज का मार्गदर्शन करेंगे ।
यदि बर्फ और मौसम की स्थिति सही रहती है तो टीम कुछ ही दिनों में वहां पहुंच सकती है । वहां दक्षिणी गर्मियों और विभिन्न आधुनिक उपकरणों की मदद से वैज्ञानिकों को काफी समय मिल जाएगा जिससे वे समुद्र के जीवों और रसायन के नमूने प्राप्त् कर सकेगे । टीम का अनुमान है कि वेडेल सागर जैसे गहरे समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र बर्फ के नीचे अंधेरे में विकसित हुआ है ।
यदि नई प्रजातियां इस क्षेत्र में बसना शुरू करती हैं, तो कुछ वर्षों के भीतर पारिस्थितिकी तंत्र में काफी बदलाव आ सकता है। गैस्ट्रोपोड्स और बाईवाल्व्स जैसे जीवों के ऊतक के समस्थानिक विश्लेषण से आइसबर्ग के टूटने के बाद से खाद्य श्रृंखला में बदलाव का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि जानवरों के ऊतकों में रसायनों की जांच से उनके आहार क ेसुराग मिल जाते हैं।
मानवीय गतिविधियों से अप्रभावित इस क्षेत्र से लिए जाने वाले नमूने शोधकर्ताओं के लिए एक अमूल्य संसाधन साबित होंगे । इस डैटा से वैज्ञानिकों को समुद्री समुदायों के विकास से जुड़े प्रश्नों को सुलझाने में तो मदद मिलेगी ही, यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि इस समुद्र के नीचे पाई जाने वाली ये प्रजातियां कितनी जल्दी बर्फीले क्षेत्र में रहने के सक्षम हो जाएंगी
क्या बिल्लियां अपना नाम पहचानती हैं ?
बिल्लियां इंसानों के प्रति थोड़े उदासीन स्वभाव के लिए जानी जाती हैं। कई बिल्लियोंके मालिकों को लगता है कि जब वे उन्हें पुकारते हैं तो वे प्रतिक्रिया नहीं देती । लेकिन हाल ही में साइंटिफिक रिपोर्टस में प्रकाशित अध्ययन कहता है कि पालतू बिल्लियां अपना नाम पहचानती हैं और पुकारे जाने पर अपना सिर घुमाकर या कान खड़े कर उस पर प्रतिक्रिया भी देती हैं।
बिल्लियांअपना नाम पहचानती हैं या नहीं? यह जानने के लिए युनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के अत्सुतो साइतो और उनके साथियों ने जानवरों के व्यवहार के अध्ययन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक की मदद से बिल्लियों पर अध्ययन किया। शोधकर्ताओं ने घरेलू पालतू बिल्लियों (फेलिस कैटस) के मालिकों से बिल्लियों के नाम से मिलती-जुलती और उतनी ही लंबी ४ संज्ञाएं पुकारने को कहा। अंत में मालिकों को बिल्ली का नाम पुकारना था ।
शोधकर्ताओं ने संज्ञाओं के पुकारे जाने पर बिल्लियों की प्रतिक्रिया का बारीकी से अध्ययन किया । उन्होंने पाया कि पहली संज्ञा पुकारे जाने पर बिल्लियों ने अपना सिर या कान घुमाकर थोड़ी-सी प्रतिक्रिया दिखाई थी लेकिन चौथी संज्ञा आते-आते बिल्लियों की प्रतिक्रिया में कमी आई थी। और जब पांचवी बार बिल्लियों का अपना नाम पुकारा गया तब ११ में से ९ बिल्लियों की प्रतिक्रिया फिर से बढ़ गई थी ।
लेकिन सिर्फ इतने से साबित नहीं होता कि वे अपना नाम पहचानती हैं। अपने नाम के प्रति प्रतिक्रिया देने के पीछे एक संभावना यह भी हो सकती है कि अन्य पुकारे गए शब्दों (नामों) की तुलना में उनके नाम वाला शब्द ज्यादा जाना-पहचाना था । इस संभावना की जांच के लिए शोधकर्ताओं ने एक और प्रयोग किया। इस बार उन्होंने उन बिल्लियों के साथ अध्ययन किया जहां एक घर में पांच या उससे ज्यादा पालतू बिल्लियां थीं । बिल्लियों के मालिकों को शुरुआती ४ नाम अन्य साथी बिल्लियों के पुकारने थे और आखिरी नाम बिल्ली का पुकारना था ।
शोधकर्ताओं ने पाया कि आखिरी नाम पुकारे जाने तक २४ में से सिर्फ ६ बिल्लियों की प्रतिक्रिया में क्रमिक कमी आई थी, अन्य बिल्लियां सभी नामों के प्रति सचेत रहीं । इस परिणाम से लगता है कि बिल्लियां जाने-पहचाने नामों (शब्दों) के साथ कोई अर्थ या इनाम मिलने की संभावना देखती हैं इसलिए सचेत रहती हैं । लेकिन अध्ययन में जिन ६ बिल्लियों ने अन्य नामों के प्रति उदासीनता दिखाई उन्होंने अपना नाम पुकारे जाने पर अत्यंत सशक्त प्रतिक्रिया दी। इससे लगता है कि कुछ बिल्लियां अपने नाम और अन्य नामों के बीच अंतर कर पाती हैं।
इस बात की पुष्टि के लिए शोधकर्ताओं ने कैट कैफे की बिल्लियों के साथ एक और अध्ययन किया, जहां लोग आकर बिल्लियों के साथ वक्त बिताते हैं। इस अध्ययन में बिल्लियों ने अपने नाम के प्रति अधिक प्रतिक्रिया दिखाई। इन सभी अध्ययनों के परिणामों के मिले-जुले विश्लेषण से लगता है कि बिल्लियों के लिए उनका अपना नाम उनके लिए कुछ महत्व रखता है। युनिवर्सिटी ऑफब्रिस्टल के जॉन ब्रेडशॉ का कहना है कि बिल्लियां कुतों की तरह सीखने में माहिर होती हैं। लेकिन उन्होंने जो सीखा उसका वे प्रदर्शन नहीं करती । ।
सुपर प्लांट जो सोख लेगा कार्बन डाई ऑक्साइड
दुनियाभर में जलवायु परिवर्तन की बढ़ रही समस्याआें से कुछ हद तक निजात पाने के लिए अमरीका के कैलिफोर्निया स्थित साल्क इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल स्टडीज की प्रोफेसर डॉ जोन चोरि ने एक नायाब तरीका खोज निकाला है ।
असल में डॉ जोन एक ऐसी योजना पर काम कर रही है जोकि पृथ्वी के तापमान को कम कर देगा । उन्होंने एक ऐसे पौधे को विकसित किया है जो वातावरण से कार्बन डाई ऑक्साइड को सोख लेगा, इससे प्रतिवर्ष ४६ फीसदी तक कार्बन की मात्रा को कम किया जा सकेगा ।
जलवायु संरक्षण को लेकर लम्बे समय से काम कर रही डॉ. जोन बताती है कि वैसे सुनने में यह बहुत ही आसान है, लेकिन जिस पौधे की हम कल्पना कर रहे हैं उससे वातावरण में तेजी से बढ़ रही कार्बन की मात्रा को कम करने का प्रयास है ।
निश्चित ही इसे जलवायु परिवर्तन की दिशा में एक सार्थक कदम के रूप में देखा जा सकता है । वैसे तो प्राकृतिक रूप से हर पौधे कार्बन का अवशोषण करके ऑक्सीजन देते हैं ।
कार्बन शोषित करने और एकत्र करने के लिए समय के साथ पौधे विकसित हुए हैं । असल में पौधों की जड़ों में सबेरिन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है जोकि कार्बन को अवशोषित करने में मदद करता है । जिस पौधे के विकास पर डॉ. जोन की टीम काम कर रही है उसकी जड़े प्राय: सामान्य पौधों से लम्बी होगी । ऐसे में ये पौधे अधिक मात्रा में कार्बन का अवशोषण कर सकेंगे ।
मौजूदा समय में साल्क इंस्टीट्यूट बीज कंपनियों के साथ बातचीत कर दुनियाभर में नौ कृषि फसलोंपर परीक्षण कर आदर्श पौधे तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है ।
गेहूं, सोयाबीन, मक् का और कपास के पौधों पर इस साल के अंत में फील्ड-टेस्टिंग शुरू हो सकती है ।
सदस्यता लें
संदेश (Atom)