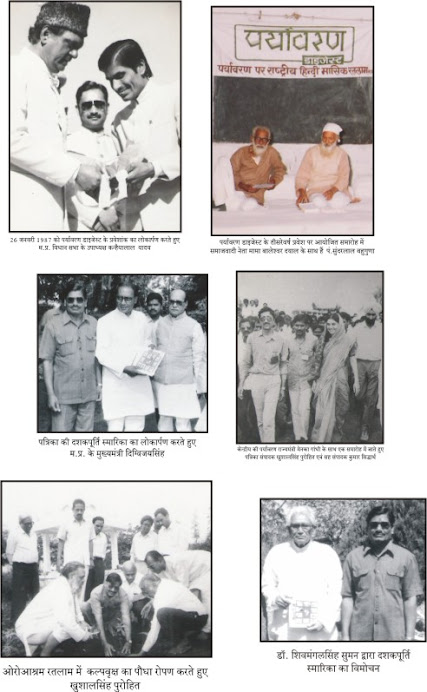आधुनिक या समावेशी विकास
डॉ.बनवारीलाल शर्मा
आजादी के बाद विकास का जो मॉडल हमने चुना है वह सभी को अपने में समाहित करने वाला नहीं था । यह समाज की ऊपरी परत को लगातार लाभ दिलवाता रहा और उसके परिणाम आज हमारे सामने हैं । देश की तीन-चौथाई आबादी के पास दो जून रोटी तक का आसरा नहीं है और दूसरी ओर एक उद्योगपति अपने परिवार के रहने के लिए २७०० करोड़ रूपये का घर बना रहा है ।
अब यह सिद्ध हो गया है कि १५ अगस्त १९४७ को औपनिवेशिक शासन से मुक्त होते समय हमने विकास का जो रास्ता अपनाया, वह गलत था । हालाँकि महात्मा गांधी उस समय जीवित थे, मगर उनकी अनसुनी करने का दुस्साहस नए देश के नए नेताआें में आ चुका था । हमारे नीति निर्माता गाँवों को पीछे छोड़ कर औद्योगीकरण की राह पर चल पड़े आर्थिक विषमता की खाई गहरानी शुरू हो गई । इस विषमता से असंतोष फैलना स्वाभाविक था, इसीलिए सन् १९७५ में भारत की जनता को इस इमर्जेंासी और उसके तहत लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन झेलना
पड़ा । इस दौर में गरीबी हटाओ का नारा भी सुनाई दिया और संविधान मेंं संशोधन कर भारत को समाजवादी गणतंत्र घोषित कर दिया गया, लेकिन वह सब जन साधारण की आँखों में धुल झोंकने के लिये था । नब्बे के दशक में हमारी सरकारों ने पूरी तरह वैश्वीकरण और आर्थिक उदारीकरण का रास्ता अपना लिया । इसके परिणामस्वरूप अब सर्वनाश एकदम सामने आ खड़ा हुआ है ।
आज एक बहुत ही खतरनाक परिदृश्य हमें दिखाई देता है । एक ओर देश की आबादी के ०.०१३ प्रतिशत, यानी सिर्फ १२ लाख लोगों के पास देश की एक तिहाई सम्पत्ति है । इन लोगों की समझ में नहीं आता कि इस ऐश्वर्य का क्या उपयोग करें । इतने धन को कैसेखर्च करें ? अत: विलास का नंगा नाच
है । दूसरी ओर मुख्यत: सरकारी, अर्द्ध सरकारी और सेवा क्षेत्र के कर्मचारियों से बना मध्यवर्ग है, जिसे संगठित होने के कारण अपनी माँगे मनवा ले जाने की सुविधा है । अत: उसका आर्थिक आधार सुरक्षित है । उदारीकरण के दौर में कॉरपोरेट जगत के लिए आबादी यह हिस्सा अत्यन्त महत्वपूर्ण है, जिसके लिये तमाम तरह की उपभोक्ता सामग्री से देश के बाजार और विज्ञापनों से समाचापत्र पटे रहते हैं । सबसे अन्त में देश के तीन चौथाई से भी अधिक ७७ प्रतिशत यानी ८४ करोड़ लोग हैं जो २० रू. या उससे भी कम प्रति दिन की आमदनी पर अपनी जिन्दगी चला रहे हैं ।
देश का हर दूसरा बच्च कुपोषित
है । चारों तरफ भूखमरी की हालत है । आश्चर्य नहीं कि इस व्यवस्था को लेकर असंतोष निरन्तर गहरा रहा है और यत्र-तत्र सर्वत्र जनता के स्वत:स्फूर्त आन्दोलन खड़े हो रहे हैं । लेकिन हमारी सरकारों में अपनी गलतियों को स्वीकार करने की सदाशयता नहीं है और उसमें सहिष्णुता की कमी भी है । वह निर्मम होकर जनान्दोलनों का क्रूर दमन करती है । शान्तिपूर्ण ढंग से किये जा रहे आन्दोलनों की इसी अनदेखी के कारण सरकारी हिंसा के विरोध में अब नक्सलवाद और माओवाद के रूप में हिंसक आन्दोलन भी अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं । क्या इन खतरनाक परिस्थितियों में अनन्त काल तक हमारा देश एकजुट और अखण्ड रह पायेगा ?
समय आ गया है कि भावी सर्वनाश से बचने के लिये समाज के जागरूक व्यक्ति तत्काल पहल करेंऔर एक नयी राजनीति और विकास का एक वैकल्पिक ढाँचा तैयार करने के लिये के लिये एकजुट हो जाएं ।
सवाल उठता है कैसा होना चाहिए हमारे विकास का मॉडल ? विकास को मात्र सकल आर्थिक वृद्धि (जीडीपी) से नहीं नापा जा सकता । हालाँकि देश में अरबपतियों की संख्या तेजी से बढ़ी है और मध्यवर्ग के एक बहुत बड़े हिस्से को भी सम्पन्नता का स्वाद चखने का मौका मिला है, मगर ऊपर के तबके की इस सम्पन्नता से कुछ छन-छन कर नीचे आयेगा और उससे गरीबी खत्म हो जायेगी यह सोचना हास्यास्पद है । समाज का सबसे आखिरी आदमी कितना खुशहाल ओर सन्तुष्ट है यही विकास का वास्तविक पैमाना हो सकता है । शोषण और असमानता पर आधारित यह विकास जो प्रकृति का विनाश कर रहा है । कदापि खुशहाली नहीं ला सकता है । यह विकास सिर्फ संविधान और कानून की दुहाई देते हुए हिंसा पैदा कर सकता है या फिर जातिभेद, लिंगभेद और साम्प्रदायिकता के नाम पर मनुष्य को मनुष्य का दुश्मन बना सकता है ।
साम्राज्य, पूँजीवाद और उपभोक्तावाद से अपनी जड़ें सींचने वाले इस विकास को हमें एक समतामूलक विकास से बदलना होगा जहाँ बाजार और मुनाफा मनुष्य की नियति तय न करें । बेलगाम उदारीकरण सार्वजनिक सम्पत्ति का निजीकरण, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, कॉरपोरेट खेती आदि से बचते हुए हमें ऐसा विकास माडल तैयार करना पड़ेगा जहाँ जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की बुनियादी जरूरतें पूरी करने की क्षमता तो हो लेकिन किसी भी व्यक्ति को असीम उपभोग की छूट न हो ।
पश्चिम की तर्ज पर किया जाने वाला विकास हमारे दशे की परिस्थितियों के कतईअनुकूल नहीं हैं । बड़े बाँध, परमाणु ऊर्जा, नदी जोड़ों परियोजना, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) आदि की हमें जरूरत नहीं है । विशालकाय उद्योगों भारी पूँजी और प्राकृतिक संसाधनों के निर्मम दोहन की बुनियाद पर खड़े विकास के स्थान पर हमारा विकास कृषि केन्द्रित होना चाहिए, जिसमें किसान को मजबूत आर्थिक आधार भी मिले और सम्मानपूर्ण जीवन भी । किसान आज की तरह अकुशल श्रमिक न कहा जाए । विकास ऐसा हो, जिसमें व्यक्ति की जरूरतों ओर प्रकृति के बीच एक सन्तुलन हो, श्रम प्रधान तकनीकी का इस्तेमाल हो व ग्रामीण, लघु व कुटीर उद्योगों की प्राथमिकता रहे । आधुनिक तकनीकी के साथ हम समयसिद्ध पारम्परिक लोक ज्ञान का उपयोग विकास के लिये करना चाहते हैं । प्राकृ तिक संसाधनों पर राज्य के स्वामित्व के सार्वभौम सत्ता के सिद्धांत को हम खारिज करते हैं और जल, जंगल, जमीन के अधिकार वापस जनता को देना चाहते हैं ।
गांधी की ग्राम गणराज्य की अवधारणा इस सर्व जन सुखाय विकास का आधार बन सकती है । ७३ वें एवं ७४ वें संविधान संशोधन अधिनियमों के रूप में हमारे पास ऐसा एक जरिया भी है । लेकिन भले ही यह कानून संसद में पारित हो गया हो, न केन्द्र सरकार ने इन कानूनों को लागू करने में विशेष रूचि ली और न अधिकांश राज्य सरकारों ने, क्योंकि ये कानून ठीक उसी वक्त शुरू किये जा रहे आर्थिक उदारीकरण के रास्ते में आड़े आ रहे थे । इन कानूनों में कुछ छिटपुट कमियाँ
हैं । उदाहरणार्थ ग्रामसभा जिसमें गाँव के सभी वयस्क शामिल होते हैं, को सर्वोच्च्ता नहीं दी गई है । यदि राजस्व ग्राम के बदले तोक गाँव या पुरवा तथा शहरों में मोहल्ले को इकाई माना जाये जिला नियोजन समिति को सचिवालय के पूरे अधिकार दे दिये जायें और केन्द्र से किसी राज्य को मिलने वाला आधे से अधिक धन ७४वें संविधान संशोघन में उल्लिखित राज्य वित्त आयोग के माध्यम से सीधे पंचायतों को दे दिया जाये तो विकास के वैकल्पिक ढाँचे की शुरूआत हो सकती
है ।
प्राकृतिक संसाधनों से यदि उत्पादन के लिये परियोजनाएं बनाने की जरूरत है तो यह कार्य उत्पादक कम्पनी बना कर किया जा सकता है । यदि ग्रामसभा किसी परियोजना से सहमत हो उससे स्थानीय समुदाय का पर्यावरण न बिगड़ता हो और न विस्थापन होता हो तो यह परियोजना स्थानीय लोग उत्पादक कम्पनी बनाकर कर सकते हैं और बाहरी पूँजी का दखल रोक सकते हैं । किसी भी तरह के विकास मेंें विस्थापन अन्तिम विकल्प होना चाहिये और उसे समाज की आम सहमति से किया जाना चाहिये । स्वावलम्बन के लिए बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर होना जरूरी है । अत: उत्पादक कम्पनियाँ बना कर देश में उपलब्ध बायोमास सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा व पानी की ऊर्जा से बिजली बना कर ग्राम समाज को आत्मनिर्भर बनाना वैकल्पिक विकास की प्राथमिकता में होगा । ताकि गाँव - गाँव में छोटे उद्योगों का जाल बिछ जाए और कॉरपोरेट ताकतों को बाहर किया जा सके ।
मगर विकास के इस वैकल्पिक मॉडल को जमीन पर उतारने के लिये एक वैकल्पिक राजनीति तैयार करना सबसे पहले जरूरी है । ***