हमारा भूमण्डल
खाद्यान्न, नीलामी की वस्तु नहीं है
ओलिवर डी शट्टर
खाद्य पदार्थ और वह भूमि जिस पर किइसे उपजाया जाता है, इतनी महत्वपूर्ण है कि उसे `मुक्त बाजार` के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता । बाजार का तो एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना है । वहीं दुनिया में कई ऐसी अनिवार्यता हैं, जिन्हें हानि लाभ के नजरिए से बाहर आकर देखना होगा । खाद्यान्न सिर्फ उसी का नहीं हो सकता जिसमें सर्वाधिक ऊंची बोली लगाने की क्षमता हो ।
खाद्यान्न, नीलामी की वस्तु नहीं है
ओलिवर डी शट्टर
खाद्य पदार्थ और वह भूमि जिस पर किइसे उपजाया जाता है, इतनी महत्वपूर्ण है कि उसे `मुक्त बाजार` के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता । बाजार का तो एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना है । वहीं दुनिया में कई ऐसी अनिवार्यता हैं, जिन्हें हानि लाभ के नजरिए से बाहर आकर देखना होगा । खाद्यान्न सिर्फ उसी का नहीं हो सकता जिसमें सर्वाधिक ऊंची बोली लगाने की क्षमता हो ।
सन् २००८ में जब वैश्विक बाजारों में खाद्य सामग्री के मूल्यों में असाधारण तेजी छाई हुई थी, ठीक उसी दौरान मैंने सं.रा. संघ के भोजन के अधिकार के विशेष दूत की भूमिका स्वीकार की । खाद्य आयात करने वाले देशों में भोजन दंगे होने लगे थे और गरीबों में भूख और गहरी पैठ करती जा रही थी, लेकिन इस सबके बावजूद एक सुनहरी लकीर भी थी । हमारी खाद्य प्रणाली के असंतुलन जो कि पिछले चालीस वर्षों में लगातार बढ़ते जा रहे एकाएक दिखाई देने लगे थे । उस ग्रीष्म ऋतु में हमें पता चला कि वैश्विक खाद्य आपूर्ति अब हमसे कुछ ही खराब फसली मौसम दूर है और हम वैश्विक मांग की पूर्ति कर पाने में असमर्थ हो जाएंगे । लेकिन इसी दौरान हमें वैश्वीकृत खाद्य प्रणाली के अन्यायकारी तर्क की झलक भी मिली और अत्यधिक व्यापक क्रय शक्ति वाला जनसमुदाय बहुत प्रभावशाली ढंग से इस सर्वकालिक अनिवार्य संसाधन की बोली लगाने में जुट गया ।
वैश्विक बाजार क्रूर कार्य-कुशलता से आवश्यकता वाले वर्ग के बजाए सबसे ज्यादा बोली लगाने वालों को संसाधन आबंटित कर देता है । यह साधारण सा जादू विकासशील देशों के बड़े क्षेत्रों में खेतों को कारों के इंर्धन के लिए चारा उपजाने या पश्चिम में मांस की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए आवश्यक पशुओं के आहार की खेती की ओर मोड़ देता है । कुछ अनुमानों के अनुसार सन् २००९ व २०१३ में मध्य यूरोपीय बायो इंर्धन कंपनियों ने अफ्रीका में करीब ६० लाख हेक्टेयर भूमि खरीदी है । यहां `अदृश्य भूमि` यूरोप के पशुओं के लिए प्रोटीन की उपलब्धता हेतु सुरक्षित है । सन् २०१० में यह २ करोड़ हेक्टेयर तक पहुंच गई थी जो कि यूरोप की अपनी कुल कृषि योग्य भूमि का १० प्रतिशत बैठती है । इतना ही नहीं छोटी प्रजातियों की मछलियां बजाए स्थानीय समुदाय द्वारा प्रयोग में लाए जाने के, हजारों किलोमीटर दूर भेजी जा रही हैं । जहां पर धन कमाने के उद्देश्य से इन्हें अमीर उपभोक्ताआें और रईसों को बेचा जा रहा है ।
अमीर देशों में बड़ी मात्रा में भोजन की बर्बादी होती है । एक यूरोपीय या उत्तरी अमेरिकी उपभोक्ता एक वर्ष में औसतन १०० किलो तक भोजन कचड़े में फेंक देता है, क्योंकि खाने पर होने वाला खर्च उनके परिवार के खर्च का बहुत छोटा हिस्सा होता है । कुल मिलाकर अमीर उपभोक्ताआेंका संसाधनों पर कब्जा बना हुआ है और उनकी जीवनशैली बिना किसी चुनौती के सतत जारी है। जबकि अन्य लोगों को अनिवार्य केलोरी तक नहीं मिल पा रही हैं और पर्यावरण पर जोखिम बढ़ता ही जा रहा है ।
वास्तव में इन बिंदुओं पर खाद्य प्रणाली आश्चर्यजनक ढंग से असफल सिद्ध हो रही है, जैसे कि करीब एक अरब लोग अभी भी भूखे हैं जबकि एक अरब चालीस करोड़ व्यक्तियों का या तो वजन ज्यादा है या वे मोटे हैं । वहीं खाद्य प्रणाली मानव निर्मित ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जन में करीब एक तिहाई का योगदान करती है । यह भी अनुमान है कि मवेशी क्षेत्र की वैश्विक ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जन में ५१ प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि इसमें मवेशियों के सांस लेने और पशु चराई हेतु वनों एवं लकड़ियों की कटाई और चारे की फसल को गिना ही नहीं गया है । इसके बावजूद अनेक लोगों का विश्वास है कि भविष्य के लिए मुख्य चुनौती वैश्विक खाद्य उत्पादन में वृद्धि ही है और बाजार के संकेतों और आपूर्ति में वृद्धि हेतु इसे और अधिक स्वतंत्रता देनी चाहिए ।
लेकिन इससे उत्पन्न हो रही समस्याओं की अनदेखी की जा रही है व वर्तमान असफलताओं की ओर से आंख मूंदी जा रही है । इसी के साथ खादों की मात्रा में लगातार बढ़ रही है और कारखाना खेती को अतिरिक्त महत्व दिया जा रहा है । हमें २१वीं सदी के लिए नए वैकल्पिक मानदंड तैयार करने की आवश्यकता है । विकासशील देश स्वमेव अपने छोटे किसानों को ऋण, तकनीक व बाजार में पहुंच संबंधी उनकी आवश्यकताओं को लेकर बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे । पर्यावरणीय दृष्टि से सुस्थिर एवं अधिक उपज देने वाले कृषि पारिस्थितिकी प्रणाली को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है और इन उत्पादकों को स्थानीय उपभोक्ताआें से जोड़ने के प्रयास किए जाने चाहिए ।
बहरहाल इन सुधारों को किसी शून्य में नहीं खड़ा किया जा सकता । हमारी वैश्विकृत खाद्य प्रणाली में सभी संकेत तो अमीर देशों के पिटारे में बंद हैं। वैश्विक दक्षिण के सुधारों की सफलता की कुंजी वैश्विक उत्तर के सुधारों में छिपी है । डेरी उत्पादों एवं जैविक इंर्धन की अपनी बढ़ती मांग में कमी लाकर व खाद्य सामग्री की बर्बादी रोककर अमीर देश उनके द्वारा विश्वभर के खेतों पर लगे कलंक को धो सकते हैं और कम क्रयशक्ति वालों को उन संसाधनों के इस्तेमाल का हक दे सकते हैं, जिनकी कि उन्हें जरूरत है ।
अमीर देशों की कृषि सब्सिडी गरीबों पर आक्रमण है : परिवर्तन तो आपूर्ति पक्ष की ओर से आना चाहिए । सवाल सिर्फ कितना उत्पादन कर रहे हैं का नहीं है बल्कि कैसे कर रहे हैं का भी है । अमीर देशों में अनाज पर मिल रही अनापशनाप सब्सिडी की वजह से हाल के दशकों में मांस एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की चांदी हो गई है । इसने विकासशील देशों को खाद्य आयात पर टिके रहने हेतु ललचाया । परंतु यह गरीब की थाली में पोषक भोजन परोस देने के लिए काफी नहीं है और इससे उन छोटे किसानों की वास्तविक आय अर्जन के अवसरों की हानि की क्षतिपूर्ति भी नहीं हो सकती, जिनके कि अपने स्थानीय बाजार में आपूर्ति के अवसर समाप्त हो जाते हैं। क्रमबद्ध तरीके से अपनी कृषि सब्सिडी में कटौती कर विकसित देश विकासशील देशों के छोटे किसानों को अपनी आजीविका एवं स्थानीय समुदायों को भोजन उपलब्ध करवाने में सहायता कर सकते हैं ।
जब इस मॉडल को सफल होने का मौका दिया जाएगा तभी विकासशील देशों को मौका मिलेगा और वे अपने छोटे खेतों को महाकाय निर्यात केन्द्रित उत्पाद इकाइयों को बेच पाने का विकल्प ढूंढ पाएंगे ।
इसके बाद ही उम्मीद की जा सकती है कि वैश्विक मूल्य इतने दयावान हो जाएंगे कि लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए अनाज खरीद पाएंगे । सन् २००८ के खाद्य संकट के छ: वर्ष बाद `कृषि में पुनर्निवेश` हुआ तो है लेकिन इसमें उत्पादन बढ़ाने के ढांचे के अलावा किसी और बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया । उत्तर और दक्षिण में सुधार के बिना और नए मानदंड निर्धारण के बगैर वैश्विक खाद्य प्रणाली `नीलामी घर` बनी रहेगी । जहां पर अमीर विश्व विलासिता का स्वाद, गरीबों की प्राथमिक आवश्यकताओं से लगातार प्रतिस्पर्धा करता रहेगा और जीतता भी रहेगा ।
वैश्विक बाजार क्रूर कार्य-कुशलता से आवश्यकता वाले वर्ग के बजाए सबसे ज्यादा बोली लगाने वालों को संसाधन आबंटित कर देता है । यह साधारण सा जादू विकासशील देशों के बड़े क्षेत्रों में खेतों को कारों के इंर्धन के लिए चारा उपजाने या पश्चिम में मांस की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए आवश्यक पशुओं के आहार की खेती की ओर मोड़ देता है । कुछ अनुमानों के अनुसार सन् २००९ व २०१३ में मध्य यूरोपीय बायो इंर्धन कंपनियों ने अफ्रीका में करीब ६० लाख हेक्टेयर भूमि खरीदी है । यहां `अदृश्य भूमि` यूरोप के पशुओं के लिए प्रोटीन की उपलब्धता हेतु सुरक्षित है । सन् २०१० में यह २ करोड़ हेक्टेयर तक पहुंच गई थी जो कि यूरोप की अपनी कुल कृषि योग्य भूमि का १० प्रतिशत बैठती है । इतना ही नहीं छोटी प्रजातियों की मछलियां बजाए स्थानीय समुदाय द्वारा प्रयोग में लाए जाने के, हजारों किलोमीटर दूर भेजी जा रही हैं । जहां पर धन कमाने के उद्देश्य से इन्हें अमीर उपभोक्ताआें और रईसों को बेचा जा रहा है ।
अमीर देशों में बड़ी मात्रा में भोजन की बर्बादी होती है । एक यूरोपीय या उत्तरी अमेरिकी उपभोक्ता एक वर्ष में औसतन १०० किलो तक भोजन कचड़े में फेंक देता है, क्योंकि खाने पर होने वाला खर्च उनके परिवार के खर्च का बहुत छोटा हिस्सा होता है । कुल मिलाकर अमीर उपभोक्ताआेंका संसाधनों पर कब्जा बना हुआ है और उनकी जीवनशैली बिना किसी चुनौती के सतत जारी है। जबकि अन्य लोगों को अनिवार्य केलोरी तक नहीं मिल पा रही हैं और पर्यावरण पर जोखिम बढ़ता ही जा रहा है ।
वास्तव में इन बिंदुओं पर खाद्य प्रणाली आश्चर्यजनक ढंग से असफल सिद्ध हो रही है, जैसे कि करीब एक अरब लोग अभी भी भूखे हैं जबकि एक अरब चालीस करोड़ व्यक्तियों का या तो वजन ज्यादा है या वे मोटे हैं । वहीं खाद्य प्रणाली मानव निर्मित ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जन में करीब एक तिहाई का योगदान करती है । यह भी अनुमान है कि मवेशी क्षेत्र की वैश्विक ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जन में ५१ प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि इसमें मवेशियों के सांस लेने और पशु चराई हेतु वनों एवं लकड़ियों की कटाई और चारे की फसल को गिना ही नहीं गया है । इसके बावजूद अनेक लोगों का विश्वास है कि भविष्य के लिए मुख्य चुनौती वैश्विक खाद्य उत्पादन में वृद्धि ही है और बाजार के संकेतों और आपूर्ति में वृद्धि हेतु इसे और अधिक स्वतंत्रता देनी चाहिए ।
लेकिन इससे उत्पन्न हो रही समस्याओं की अनदेखी की जा रही है व वर्तमान असफलताओं की ओर से आंख मूंदी जा रही है । इसी के साथ खादों की मात्रा में लगातार बढ़ रही है और कारखाना खेती को अतिरिक्त महत्व दिया जा रहा है । हमें २१वीं सदी के लिए नए वैकल्पिक मानदंड तैयार करने की आवश्यकता है । विकासशील देश स्वमेव अपने छोटे किसानों को ऋण, तकनीक व बाजार में पहुंच संबंधी उनकी आवश्यकताओं को लेकर बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे । पर्यावरणीय दृष्टि से सुस्थिर एवं अधिक उपज देने वाले कृषि पारिस्थितिकी प्रणाली को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है और इन उत्पादकों को स्थानीय उपभोक्ताआें से जोड़ने के प्रयास किए जाने चाहिए ।
बहरहाल इन सुधारों को किसी शून्य में नहीं खड़ा किया जा सकता । हमारी वैश्विकृत खाद्य प्रणाली में सभी संकेत तो अमीर देशों के पिटारे में बंद हैं। वैश्विक दक्षिण के सुधारों की सफलता की कुंजी वैश्विक उत्तर के सुधारों में छिपी है । डेरी उत्पादों एवं जैविक इंर्धन की अपनी बढ़ती मांग में कमी लाकर व खाद्य सामग्री की बर्बादी रोककर अमीर देश उनके द्वारा विश्वभर के खेतों पर लगे कलंक को धो सकते हैं और कम क्रयशक्ति वालों को उन संसाधनों के इस्तेमाल का हक दे सकते हैं, जिनकी कि उन्हें जरूरत है ।
अमीर देशों की कृषि सब्सिडी गरीबों पर आक्रमण है : परिवर्तन तो आपूर्ति पक्ष की ओर से आना चाहिए । सवाल सिर्फ कितना उत्पादन कर रहे हैं का नहीं है बल्कि कैसे कर रहे हैं का भी है । अमीर देशों में अनाज पर मिल रही अनापशनाप सब्सिडी की वजह से हाल के दशकों में मांस एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की चांदी हो गई है । इसने विकासशील देशों को खाद्य आयात पर टिके रहने हेतु ललचाया । परंतु यह गरीब की थाली में पोषक भोजन परोस देने के लिए काफी नहीं है और इससे उन छोटे किसानों की वास्तविक आय अर्जन के अवसरों की हानि की क्षतिपूर्ति भी नहीं हो सकती, जिनके कि अपने स्थानीय बाजार में आपूर्ति के अवसर समाप्त हो जाते हैं। क्रमबद्ध तरीके से अपनी कृषि सब्सिडी में कटौती कर विकसित देश विकासशील देशों के छोटे किसानों को अपनी आजीविका एवं स्थानीय समुदायों को भोजन उपलब्ध करवाने में सहायता कर सकते हैं ।
जब इस मॉडल को सफल होने का मौका दिया जाएगा तभी विकासशील देशों को मौका मिलेगा और वे अपने छोटे खेतों को महाकाय निर्यात केन्द्रित उत्पाद इकाइयों को बेच पाने का विकल्प ढूंढ पाएंगे ।
इसके बाद ही उम्मीद की जा सकती है कि वैश्विक मूल्य इतने दयावान हो जाएंगे कि लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए अनाज खरीद पाएंगे । सन् २००८ के खाद्य संकट के छ: वर्ष बाद `कृषि में पुनर्निवेश` हुआ तो है लेकिन इसमें उत्पादन बढ़ाने के ढांचे के अलावा किसी और बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया । उत्तर और दक्षिण में सुधार के बिना और नए मानदंड निर्धारण के बगैर वैश्विक खाद्य प्रणाली `नीलामी घर` बनी रहेगी । जहां पर अमीर विश्व विलासिता का स्वाद, गरीबों की प्राथमिक आवश्यकताओं से लगातार प्रतिस्पर्धा करता रहेगा और जीतता भी रहेगा ।





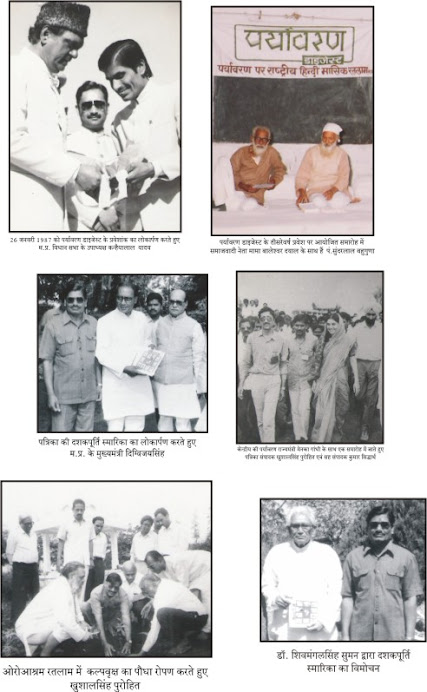



कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें