विशेष लेख
परम्पराएं, आधुनिकता और पर्यावरण
डॉ. सुनील कुमार अग्रवाल
पर्यावरण शब्द अब लोक मानस के लिए नया नहींहै और उसकी सार्थकता से भी हम अनजान नहीं है। परम्पराआें के प्रकल्प में ही लोक जीवन चला आ रहा है । परम्पराएं सदा वर्तमान की गोद में पलती है । (यह बात अलग है कि वर्तमान प्रतिपल भूत में विलीन होता है) परम्पराएं आधुनिकता के कलेवर में और भी अधिक परिष्कृत होती है । किन्तु यदि आधुनिकता के ताने बाने से संवेदना कही छीजकर या छनकर दूर हो जाती है तो परम्पराएं टूट जाती है । यही टूटन तो पर्यावरण और परिवेश परिकर में घुटन का कारण बनती है ।
आधुनिक होना बुरा नहीं है । सभ्यता की सीढ़िया चढ़ना भी बुरा नहीं है क्योंकि इससे आत्मानुशासन और आत्मैक्यता बढ़ती है । आधुनिकता तो हमारे जीवन दर्शन को नित नया आयाम देती है । नई दृष्टि देती है और मोहब्बत का पैगाम देती है । रवीन्द्र नाथ टेगोर के अनुसार भी विश्व को आसक्त भाव से न निहार कर निर्विकार तद्भव भाव से देखना आधुनिकता है ।
आधुनिकता आनंद सम्मोहिता एवं आनंदमत्ता होती है । आधारभूत, आधारशक्ति (शक्ति रूपा प्रकृति माया) पर ही आधुनिकता का आनुषंगिक महल खड़ा होता है जहाँ प्रेम रहता है । व्यष्टि को समष्टि और सृष्टि के प्रति प्रेमातुर होना ही चाहिए । प्रेम का प्रयोजन सिद्ध भी होना चाहिए क्योंकि प्रेम परसार (रसीप्रोकेट) होता है । हमारा हर क्रिया कलाप सृष्टि और पर्यावरण के प्रति प्रयोगधर्मी होना चाहिए । हमें प्रासंगिकता के साथ कदम ताल करना चाहिए । हमें परम्परा के पाथेय को समझना चाहिए और सदैव ही परिवेशगत रहना चाहिए ।
पर्यावरण का उदबोध यही है कि हम परम्परा के पाथेय पर नई दृष्टि एवं सर्जनात्मकता के साथ चलें। सृजन की प्रेरणा प्रकृति से मिलती है । परम्परा ही प्रीति की प्रस्तावक है । नवीन के प्रति आकर्षक सहज ही होता है किन्तु पुराने को भी तो कोई समझदार यकायक नहींखोता है । परम्पराएं अनेक परिवर्तनों के बीच से गुजर कर पल्लवित पुष्पित तथा सुवासित होती है । इस प्रक्रिया में वक्त लगता है जो परिवर्तन ग्राह्य नहीं होते हैं वह रूढ़ि कहलाते है । अत: हमें परम्परा और रूढ़ि में भेददृष्टि रखनी होगी । हर परम्परा बारंबार प्रासंगिकता के निकष पर कसनी होगी । प्रकृति एवं पर्यावरण पोषिता मिथकीय परम्पराएं भी सार्थक सिद्ध रही हैं । परम्परा पोषी आधुनिकता ही हमारे पर्यावरण का संबल है ।
परम्पराआें तथा समकालीन परिस्थितियों पर सम्यक चिंतन और विवेचन जरूरी है । देशकाल परिस्थितियों के अनुसार संवेदन तथा मूल्यबोध विकसित होता है । मनीषियों के अनुसार आधुनिकता स्वयं भी मूल्यों की प्रस्तोता एवं जननी है जो कि मूल्यों को प्रतिवर्ती दृष्टि भी देती है । यह मूल्य पारम्परिक होते है जिनमें समकालिक प्रवृत्तियाँ पनपती हैं । यह प्रवृत्तियाँ पर्यावरण की पोषक होनी चाहिए न कि उसकी शोषक । यह प्रवृत्तियां पर्यावरण की शोधक होनी चाहिए न कि प्रदूषक ।
हमें परम्परा के निर्वहन के नाम पर संकीर्ण रूढ़िवाद तथा आधुनिकता के नाम पर उद्दंड - उंदृखलता से सावधान रहना होगा क्योंकि दोनों ही प्रवृत्तियाँ पर्यावरण के लिए घातक है । हमें लोक हितकारी लोकायित धर्म निभाना चाहिए । दूसरों के काम आना, सुख-दुख में साथ निभाना, हाथ बंटाना आदि कर्म, लोक धर्म है । सामुहिकता ही प्रकृति एवं पर्यावरण का मूल तत्व है । हमें परम्पराआें का सम्यक मूल्यांकन भी करते रहना चाहिए तथा स्वस्थ्य परम्पराआें को जीवंत रखना चाहिए ।
हमारी सांस्कृतिक परम्पराएं आरण्यक रहीं, जिनमें प्रेमास्पद सौन्दर्यता तथा नेतृत्व सदैव रहा । परम्पराआें के मानवीय पक्ष की प्रतिष्ठा रही । अब आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता के पाथ पर मानवीय पक्ष छीज रहा है क्योंछीज रहा है ? यही यक्ष प्रश्न है जिसके उत्तर की तलाश में है हम । परम्पराएं तो सरस धारा बन कर हमारी तृष्णा को संतृप्त् करती रही हैं वैसे ही जैसे वन-प्रांतर को सरस सलिलाएं समासक्त रखती है । हमें सरसता को शुष्क एवं रूक्ष नहीं होने देना है । मधुरता के साथ सतरंगी इंद्रधनुषी भाव संजोना है ।
हमारी चिंता परम्पराआें के उस आधुनिक एवं उत्तर आधुनिक रंग में रंगने से नहीं है जो समय की मांग के अनुरूप है । कैनवास में नये-नये शेड्स भी अच्छे लगते है किन्तु हमारी चिंता उन वीभत्सताआें को लेकर अवश्य है जो कुतर्को के सहारे हरित विश्वास को धकिया रही है । और प्रकृति की नैसर्गिकता को तोड़ रही है । प्रकृति को छेड़ रही है । उन कुत्साआें से है जो परिवेश को विषाक्त कर रही हैं । उस अवमूल्यन से है जो अच्छे बुरे का भेद भूल रहा है क्योंकि केन्द्र में धन ऐश्वर्य हैं जिसके ईदगिर्द उत्तर आधुनिकता के प्रेत नृत्य कर रहे है और नई नई परिभाषाआें को गढ़ रहे हैं । हमें उनके विनाशक नृत्य को रोकना ही होगा ।
परम्परा को वर्जित मानते हुए विकास विरोधी समझना बड़ी भूल है । परम्पराएँ तो प्रगति की प्रस्तावक प्रशस्थक तथा प्रशंसक है । परम्पराएँ पर्यावरण पर दृष्टि तो रखती ही हैं साथ ही उसे पुष्ट भी करती है । प्रकृति में कुछ भी स्थाई नहीं है । प्रकृति में प्रगति है, परिवर्तन है । परिवर्तन परम्परा को सदैव नई अर्थवत्ता के साथ आगे बढ़ाता है । वरणीय आगे बढ़ जाता है । अस्वीकार पीछे टूट जाता है । चिंता यह है कि कही कभी भी हम अपनी अद्वमन्यता में वरणीय का तिरस्कार न कर दे । परम्परा को अस्वीकार न कर दें । हमारी प्रगति पारम्परिक विचारों से ही अनुप्राणित होती है ।
परम्परा तो सुदीर्घकालिक होती है । गत्यात्मकता जिसका नैसर्गिक गुण होता है जिसमें वरणेय गत्यात्मकता नहीं होती वह रूढ़ि कहलाती है । हमें रूढ़िगत नहीं वरन् प्रगतिशील समुन्नत सुविचारित पर्यावरणीय दृष्टि रखनी चाहिए । परम्परा प्रवाह है तो आधुनिकता उसकी तरणता, और वही उसकी तारन हार भी है । आदिम से आधुनिक होने की अपनी परम्परा में प्रकृति और संस्कृति का समादर करना ही होगा । आधुनिकता में हम कभी भी कहीं भी अपनी मौलिकता न छोड़े । तथ्यों को स्वार्थान्धता में न तोड़े-मरोड़े । हम अपनी प्रकृति पर आघात न करें । प्रकृति ने हमें जीवन दिया है हम प्रकृति के लिए मरना सीखें ।
देश में संस्कृतिकी जड़े गहराई तक जमी है इसके बावजूद हम गंदगी ढो रहे है । इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम अनात्म हो रहे है । हमारी आत्मा मर रही है । अपनी जड़ों से कट रहे हैं हम । हम आयातित को अपना रहे हैं, अपनी अस्मिता को भूलते जा रहे है । हम आततायी और अत्मीय का भेद भी भूल गए है । आदिम से आधुनिक हुए, अब उत्तर आधुनिकता की ओर बढ़ रहे है । यह कहॅूं तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगा कि स्वयं को स्वयं से छल रहे हैं । उत्तर आधुनिक विदूषता की सलीब को कांधों पर उठाये मर रहा है पर्यावरण । चारों ओर हो रहा है सुचिता का ही हरण । हमारी सेाच बड़ी ही सोचनीय हो गई है । अब तो उच्च् स्तरीय जीवन से उच्च् स्तरीय सोच विचार की भी गारंटी नहीं है क्योंकि सोच विचार पूरी तरह स्वार्थ से जुड़ गया है ।
हमारे पास अकूत प्राकृतिक सम्पदा है किन्तु इसे मुक्त हस्त से लुटने को भी स्वतंत्रता है । तभी तो लुटे पिटे पर्यावरण के घेरे में है हम । हमारे अंदर उलझन, अनिर्णय एवं असंतोष समाया रहता है । यूँ तो हम भाव विभोर होकर गाते-बजाते है - गो धन गज धन बाजिधन और रतनधन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान । किन्तु संतोष होता कहाँ है । आधी मिले तो आदमी पूरी के लिए दौड़ता है । वह अपनी तृष्णा कभी नहीं छोड़ता है । हम नैतिकता से दूर है, क्रूर है । हम स्वार्थी है तभी तो हमें खुशी नहीं मिलती है । एक खालीपन और रिक्तता घेरे रहती है हमें हरदम । भीड़ में भी आदमी अकेला है । यही तो उत्तर आधुनिकता का खेल है ।
वर्तमान में हम संस्कार एवं संस्कृति के स्तर पर उत्तर आधुनिकता विकास आपदा से जूझ रहे है । आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण और उपभोक्तावाद ने हमें हमारी जड़ों से काटकर वह आकाश कुसुम दिखला दिया है जो हमारी निगाह को तप्त् सूर्य के नजदीक ले आया है । झुलसते हुए भी हम उसे देखना ही नहीं, पकड़ना चाह रहे है । अपने ऐश्वर्यपूर्ण जीवन की जद्दोजहद में हम अपनी धरती आकाश और रक्षा आवरण को ही नष्ट करते आ रहे है, छटपटा रहे हैं । ऐसे में आत्म विश्वास की जरूरत है । इस तरह भला अमृर्त्य कब तक रहेगें हम ?
अत: अब वक्त आ गया है कि हम अपनी पोषिता को पहचाने अपनी प्रकृति की माने । अपनी जड़ों को पहचाने । अपने बीज को पकड़े अपने लक्ष्य को देखे । अपने संभावनाशील पंखों को खोले, संवेदी बने, उड़ान भरें, गलत से नहीं डरें । नैतिक एवं आध्यात्मिक हो जायें और अपने विश्वास को मजबूत बनाये । सर्वहारा हो जायें और अपनी संस्कृति का हर द्वार खुला पाये । मिथकीय परम्पराएं भी कही न कहीं यथार्थ से जुड़ी होती है, उस यथार्थ की तह तक जायें ।
यह निर्विवाद सत्य है कि समय की शिला पर परम्परा नित्य नये-नये प्रतिमान गढ़ती है और आधुनिकता कालान्तर में परम्परा का रूप धरती है । फिर नई आधुनातन अवस्था आती है । परिवर्तन तो जीवन की थाती है । हम कहीं भी और कभी भी अंधानुकरण न करें किन्तु सही का वरण अवश्य करें । हमारी पर्वोत्सव परम्पराएं एवं हमारी सभ्यता, संस्कृति का अंग रही पेड़-पौधों एवं जीव जन्तुआें में देवाधिष्ठान परिकल्पानाएं पर्यावरण की रक्षक है । हमारी ग्राम्या कृषि प्रधान संस्कृति सदैव वरणीय है । हम गोपद के पूजक हैं । आधुनिकता का अर्थ यह कदापि नहीं है कि हम भारतीय यशगान न भूले । वैदिक संस्कृतिको भूलकर पाश्चात्य विकृतियों को पूजने लगें । अंत में यही कहूंगा कि हम अपनी पहचान न भूले ।
परम्पराएं, आधुनिकता और पर्यावरण
डॉ. सुनील कुमार अग्रवाल
पर्यावरण शब्द अब लोक मानस के लिए नया नहींहै और उसकी सार्थकता से भी हम अनजान नहीं है। परम्पराआें के प्रकल्प में ही लोक जीवन चला आ रहा है । परम्पराएं सदा वर्तमान की गोद में पलती है । (यह बात अलग है कि वर्तमान प्रतिपल भूत में विलीन होता है) परम्पराएं आधुनिकता के कलेवर में और भी अधिक परिष्कृत होती है । किन्तु यदि आधुनिकता के ताने बाने से संवेदना कही छीजकर या छनकर दूर हो जाती है तो परम्पराएं टूट जाती है । यही टूटन तो पर्यावरण और परिवेश परिकर में घुटन का कारण बनती है ।
आधुनिक होना बुरा नहीं है । सभ्यता की सीढ़िया चढ़ना भी बुरा नहीं है क्योंकि इससे आत्मानुशासन और आत्मैक्यता बढ़ती है । आधुनिकता तो हमारे जीवन दर्शन को नित नया आयाम देती है । नई दृष्टि देती है और मोहब्बत का पैगाम देती है । रवीन्द्र नाथ टेगोर के अनुसार भी विश्व को आसक्त भाव से न निहार कर निर्विकार तद्भव भाव से देखना आधुनिकता है ।
आधुनिकता आनंद सम्मोहिता एवं आनंदमत्ता होती है । आधारभूत, आधारशक्ति (शक्ति रूपा प्रकृति माया) पर ही आधुनिकता का आनुषंगिक महल खड़ा होता है जहाँ प्रेम रहता है । व्यष्टि को समष्टि और सृष्टि के प्रति प्रेमातुर होना ही चाहिए । प्रेम का प्रयोजन सिद्ध भी होना चाहिए क्योंकि प्रेम परसार (रसीप्रोकेट) होता है । हमारा हर क्रिया कलाप सृष्टि और पर्यावरण के प्रति प्रयोगधर्मी होना चाहिए । हमें प्रासंगिकता के साथ कदम ताल करना चाहिए । हमें परम्परा के पाथेय को समझना चाहिए और सदैव ही परिवेशगत रहना चाहिए ।
पर्यावरण का उदबोध यही है कि हम परम्परा के पाथेय पर नई दृष्टि एवं सर्जनात्मकता के साथ चलें। सृजन की प्रेरणा प्रकृति से मिलती है । परम्परा ही प्रीति की प्रस्तावक है । नवीन के प्रति आकर्षक सहज ही होता है किन्तु पुराने को भी तो कोई समझदार यकायक नहींखोता है । परम्पराएं अनेक परिवर्तनों के बीच से गुजर कर पल्लवित पुष्पित तथा सुवासित होती है । इस प्रक्रिया में वक्त लगता है जो परिवर्तन ग्राह्य नहीं होते हैं वह रूढ़ि कहलाते है । अत: हमें परम्परा और रूढ़ि में भेददृष्टि रखनी होगी । हर परम्परा बारंबार प्रासंगिकता के निकष पर कसनी होगी । प्रकृति एवं पर्यावरण पोषिता मिथकीय परम्पराएं भी सार्थक सिद्ध रही हैं । परम्परा पोषी आधुनिकता ही हमारे पर्यावरण का संबल है ।
परम्पराआें तथा समकालीन परिस्थितियों पर सम्यक चिंतन और विवेचन जरूरी है । देशकाल परिस्थितियों के अनुसार संवेदन तथा मूल्यबोध विकसित होता है । मनीषियों के अनुसार आधुनिकता स्वयं भी मूल्यों की प्रस्तोता एवं जननी है जो कि मूल्यों को प्रतिवर्ती दृष्टि भी देती है । यह मूल्य पारम्परिक होते है जिनमें समकालिक प्रवृत्तियाँ पनपती हैं । यह प्रवृत्तियाँ पर्यावरण की पोषक होनी चाहिए न कि उसकी शोषक । यह प्रवृत्तियां पर्यावरण की शोधक होनी चाहिए न कि प्रदूषक ।
हमें परम्परा के निर्वहन के नाम पर संकीर्ण रूढ़िवाद तथा आधुनिकता के नाम पर उद्दंड - उंदृखलता से सावधान रहना होगा क्योंकि दोनों ही प्रवृत्तियाँ पर्यावरण के लिए घातक है । हमें लोक हितकारी लोकायित धर्म निभाना चाहिए । दूसरों के काम आना, सुख-दुख में साथ निभाना, हाथ बंटाना आदि कर्म, लोक धर्म है । सामुहिकता ही प्रकृति एवं पर्यावरण का मूल तत्व है । हमें परम्पराआें का सम्यक मूल्यांकन भी करते रहना चाहिए तथा स्वस्थ्य परम्पराआें को जीवंत रखना चाहिए ।
हमारी सांस्कृतिक परम्पराएं आरण्यक रहीं, जिनमें प्रेमास्पद सौन्दर्यता तथा नेतृत्व सदैव रहा । परम्पराआें के मानवीय पक्ष की प्रतिष्ठा रही । अब आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता के पाथ पर मानवीय पक्ष छीज रहा है क्योंछीज रहा है ? यही यक्ष प्रश्न है जिसके उत्तर की तलाश में है हम । परम्पराएं तो सरस धारा बन कर हमारी तृष्णा को संतृप्त् करती रही हैं वैसे ही जैसे वन-प्रांतर को सरस सलिलाएं समासक्त रखती है । हमें सरसता को शुष्क एवं रूक्ष नहीं होने देना है । मधुरता के साथ सतरंगी इंद्रधनुषी भाव संजोना है ।
हमारी चिंता परम्पराआें के उस आधुनिक एवं उत्तर आधुनिक रंग में रंगने से नहीं है जो समय की मांग के अनुरूप है । कैनवास में नये-नये शेड्स भी अच्छे लगते है किन्तु हमारी चिंता उन वीभत्सताआें को लेकर अवश्य है जो कुतर्को के सहारे हरित विश्वास को धकिया रही है । और प्रकृति की नैसर्गिकता को तोड़ रही है । प्रकृति को छेड़ रही है । उन कुत्साआें से है जो परिवेश को विषाक्त कर रही हैं । उस अवमूल्यन से है जो अच्छे बुरे का भेद भूल रहा है क्योंकि केन्द्र में धन ऐश्वर्य हैं जिसके ईदगिर्द उत्तर आधुनिकता के प्रेत नृत्य कर रहे है और नई नई परिभाषाआें को गढ़ रहे हैं । हमें उनके विनाशक नृत्य को रोकना ही होगा ।
परम्परा को वर्जित मानते हुए विकास विरोधी समझना बड़ी भूल है । परम्पराएँ तो प्रगति की प्रस्तावक प्रशस्थक तथा प्रशंसक है । परम्पराएँ पर्यावरण पर दृष्टि तो रखती ही हैं साथ ही उसे पुष्ट भी करती है । प्रकृति में कुछ भी स्थाई नहीं है । प्रकृति में प्रगति है, परिवर्तन है । परिवर्तन परम्परा को सदैव नई अर्थवत्ता के साथ आगे बढ़ाता है । वरणीय आगे बढ़ जाता है । अस्वीकार पीछे टूट जाता है । चिंता यह है कि कही कभी भी हम अपनी अद्वमन्यता में वरणीय का तिरस्कार न कर दे । परम्परा को अस्वीकार न कर दें । हमारी प्रगति पारम्परिक विचारों से ही अनुप्राणित होती है ।
परम्परा तो सुदीर्घकालिक होती है । गत्यात्मकता जिसका नैसर्गिक गुण होता है जिसमें वरणेय गत्यात्मकता नहीं होती वह रूढ़ि कहलाती है । हमें रूढ़िगत नहीं वरन् प्रगतिशील समुन्नत सुविचारित पर्यावरणीय दृष्टि रखनी चाहिए । परम्परा प्रवाह है तो आधुनिकता उसकी तरणता, और वही उसकी तारन हार भी है । आदिम से आधुनिक होने की अपनी परम्परा में प्रकृति और संस्कृति का समादर करना ही होगा । आधुनिकता में हम कभी भी कहीं भी अपनी मौलिकता न छोड़े । तथ्यों को स्वार्थान्धता में न तोड़े-मरोड़े । हम अपनी प्रकृति पर आघात न करें । प्रकृति ने हमें जीवन दिया है हम प्रकृति के लिए मरना सीखें ।
देश में संस्कृतिकी जड़े गहराई तक जमी है इसके बावजूद हम गंदगी ढो रहे है । इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम अनात्म हो रहे है । हमारी आत्मा मर रही है । अपनी जड़ों से कट रहे हैं हम । हम आयातित को अपना रहे हैं, अपनी अस्मिता को भूलते जा रहे है । हम आततायी और अत्मीय का भेद भी भूल गए है । आदिम से आधुनिक हुए, अब उत्तर आधुनिकता की ओर बढ़ रहे है । यह कहॅूं तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगा कि स्वयं को स्वयं से छल रहे हैं । उत्तर आधुनिक विदूषता की सलीब को कांधों पर उठाये मर रहा है पर्यावरण । चारों ओर हो रहा है सुचिता का ही हरण । हमारी सेाच बड़ी ही सोचनीय हो गई है । अब तो उच्च् स्तरीय जीवन से उच्च् स्तरीय सोच विचार की भी गारंटी नहीं है क्योंकि सोच विचार पूरी तरह स्वार्थ से जुड़ गया है ।
हमारे पास अकूत प्राकृतिक सम्पदा है किन्तु इसे मुक्त हस्त से लुटने को भी स्वतंत्रता है । तभी तो लुटे पिटे पर्यावरण के घेरे में है हम । हमारे अंदर उलझन, अनिर्णय एवं असंतोष समाया रहता है । यूँ तो हम भाव विभोर होकर गाते-बजाते है - गो धन गज धन बाजिधन और रतनधन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान । किन्तु संतोष होता कहाँ है । आधी मिले तो आदमी पूरी के लिए दौड़ता है । वह अपनी तृष्णा कभी नहीं छोड़ता है । हम नैतिकता से दूर है, क्रूर है । हम स्वार्थी है तभी तो हमें खुशी नहीं मिलती है । एक खालीपन और रिक्तता घेरे रहती है हमें हरदम । भीड़ में भी आदमी अकेला है । यही तो उत्तर आधुनिकता का खेल है ।
वर्तमान में हम संस्कार एवं संस्कृति के स्तर पर उत्तर आधुनिकता विकास आपदा से जूझ रहे है । आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण और उपभोक्तावाद ने हमें हमारी जड़ों से काटकर वह आकाश कुसुम दिखला दिया है जो हमारी निगाह को तप्त् सूर्य के नजदीक ले आया है । झुलसते हुए भी हम उसे देखना ही नहीं, पकड़ना चाह रहे है । अपने ऐश्वर्यपूर्ण जीवन की जद्दोजहद में हम अपनी धरती आकाश और रक्षा आवरण को ही नष्ट करते आ रहे है, छटपटा रहे हैं । ऐसे में आत्म विश्वास की जरूरत है । इस तरह भला अमृर्त्य कब तक रहेगें हम ?
अत: अब वक्त आ गया है कि हम अपनी पोषिता को पहचाने अपनी प्रकृति की माने । अपनी जड़ों को पहचाने । अपने बीज को पकड़े अपने लक्ष्य को देखे । अपने संभावनाशील पंखों को खोले, संवेदी बने, उड़ान भरें, गलत से नहीं डरें । नैतिक एवं आध्यात्मिक हो जायें और अपने विश्वास को मजबूत बनाये । सर्वहारा हो जायें और अपनी संस्कृति का हर द्वार खुला पाये । मिथकीय परम्पराएं भी कही न कहीं यथार्थ से जुड़ी होती है, उस यथार्थ की तह तक जायें ।
यह निर्विवाद सत्य है कि समय की शिला पर परम्परा नित्य नये-नये प्रतिमान गढ़ती है और आधुनिकता कालान्तर में परम्परा का रूप धरती है । फिर नई आधुनातन अवस्था आती है । परिवर्तन तो जीवन की थाती है । हम कहीं भी और कभी भी अंधानुकरण न करें किन्तु सही का वरण अवश्य करें । हमारी पर्वोत्सव परम्पराएं एवं हमारी सभ्यता, संस्कृति का अंग रही पेड़-पौधों एवं जीव जन्तुआें में देवाधिष्ठान परिकल्पानाएं पर्यावरण की रक्षक है । हमारी ग्राम्या कृषि प्रधान संस्कृति सदैव वरणीय है । हम गोपद के पूजक हैं । आधुनिकता का अर्थ यह कदापि नहीं है कि हम भारतीय यशगान न भूले । वैदिक संस्कृतिको भूलकर पाश्चात्य विकृतियों को पूजने लगें । अंत में यही कहूंगा कि हम अपनी पहचान न भूले ।




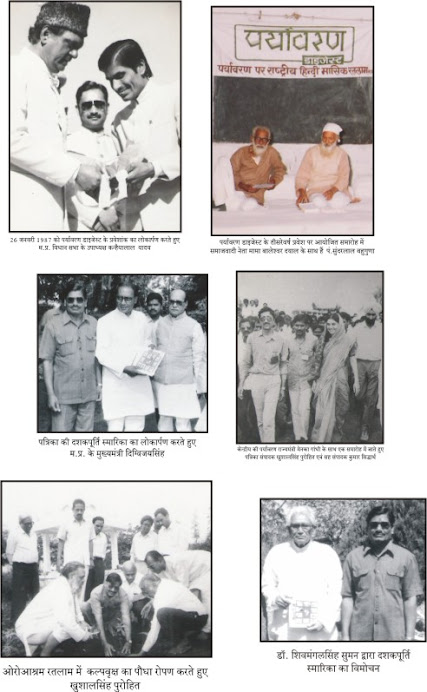



कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें